मनुस्मृति भारतीय इतिहास और समाजशास्त्र का एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो सदियों से गहन अध्ययन, विवाद और विमर्श का केंद्र रहा है। इसे अक्सर हिंदू धर्म के कानूनों और सामाजिक व्यवस्था का आधारभूत स्रोत माना जाता है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे नैतिकता, न्याय, कर्तव्य और सामाजिक श्रेणियों के नियम विस्तार से वर्णित हैं। आज भी, इसके कुछ प्रावधानों को लेकर तीखी बहस छिड़ी रहती है, खासकर जब समकालीन मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के संदर्भ में इसकी व्याख्या की जाती है। यह केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक जीवंत विषय है जो आधुनिक भारत में भी अपनी छाप छोड़ता है, चाहे वह न्यायिक संदर्भों में हो या सामाजिक सुधार आंदोलनों में। इसकी जटिल विरासत को समझने के लिए, हमें इसके मूल स्वरूप और समय के साथ इसकी बदलती व्याख्याओं को जानना आवश्यक है।
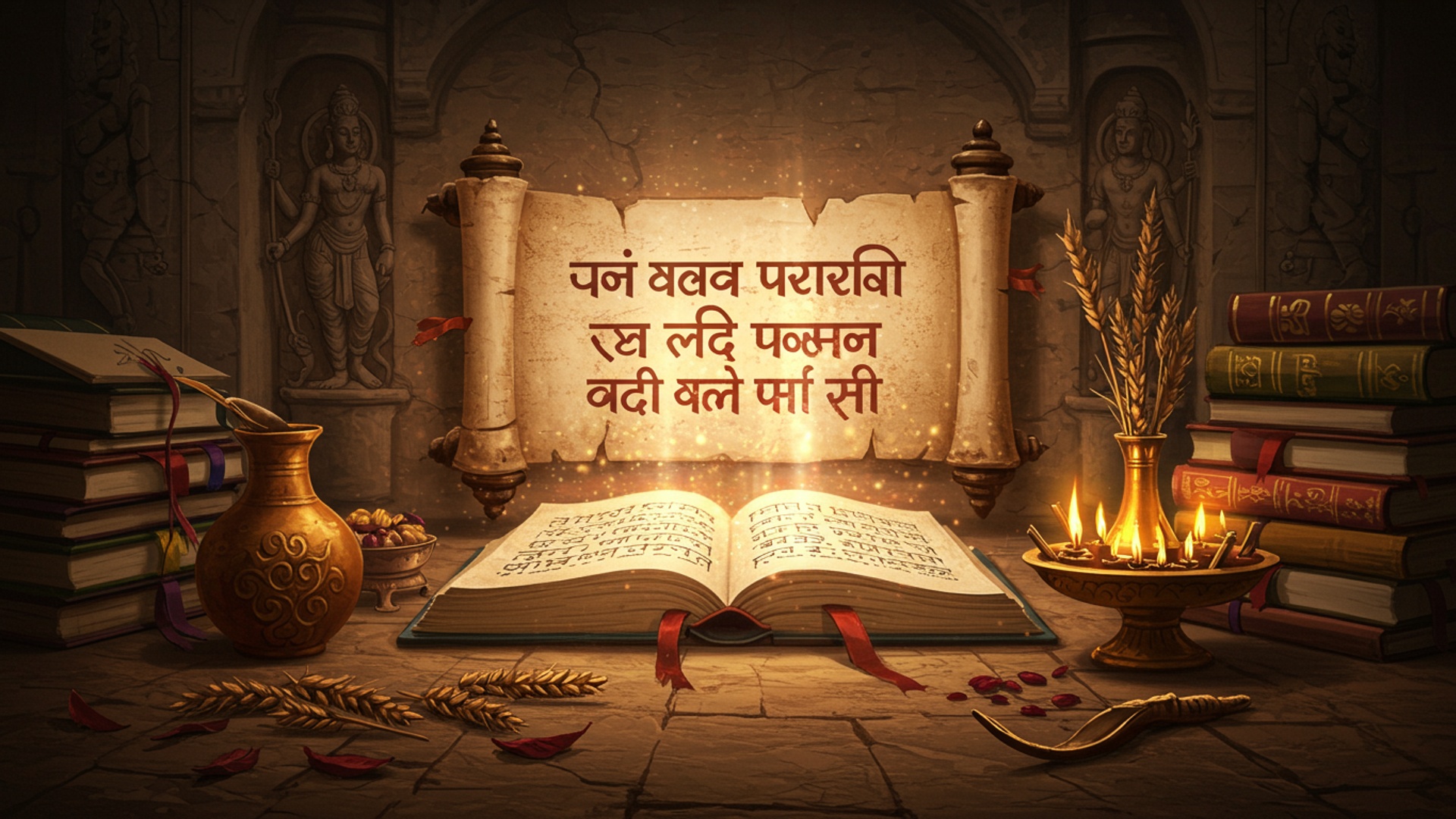
मनुस्मृति क्या है और इसका उद्भव कैसे हुआ?
नमस्ते! आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास और समाज में गहरा प्रभाव रखता है – मनुस्मृति। सरल शब्दों में कहें तो, मनुस्मृति (या ‘मनु के नियम’) हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र ग्रंथ का हिस्सा है। इसे अक्सर प्राचीन भारत की कानून संहिता के रूप में जाना जाता है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए नियम और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं।
इसके उद्भव को लेकर कई मत हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से इसे पहले मानव और ऋषि ‘मनु’ द्वारा रचित माना जाता है। हालाँकि, आधुनिक शोधकर्ता इसे एक व्यक्ति की बजाय विभिन्न कालों में विभिन्न ऋषियों द्वारा संकलित एक ग्रंथ मानते हैं। इसकी रचना का समयकाल आमतौर पर 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है, लेकिन इसके कुछ अंश पहले या बाद के भी हो सकते हैं। यह ‘स्मृति’ ग्रंथों की श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ है ‘याद किया गया’ या परंपरा पर आधारित। यह श्रुति (जैसे वेद) से भिन्न है, जिसे प्रत्यक्ष ‘सुना गया’ या ईश्वरीय रहस्योद्घाटन माना जाता है।
मनुस्मृति केवल कानूनों का संग्रह नहीं है; यह धर्म, नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तिगत कर्तव्य और राज्य-शासन के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालती है।
मनुस्मृति की संरचना और मुख्य विषय
मनुस्मृति एक विशाल ग्रंथ है जो लगभग 2684 श्लोकों (छंदों) में विभाजित है, जिन्हें 12 अध्यायों में बांटा गया है। इसकी संरचना अत्यंत व्यवस्थित है, जिसमें जीवन के हर पहलू को कवर करने का प्रयास किया गया है। आइए, इसके मुख्य अध्यायों और उनमें समाहित विषयों पर एक नज़र डालें:
- प्रथम अध्याय (सृष्टि की उत्पत्ति): इसमें ब्रह्मांड, देवताओं और मनुष्यों की उत्पत्ति का वर्णन है, जिसमें मनु को सृष्टि के पहले राजा और विधि-निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- द्वितीय अध्याय (संस्कार और ब्रह्मचर्य): इस भाग में जन्म से लेकर शिक्षा तक के संस्कारों, विशेषकर उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार और विद्यार्थी जीवन (ब्रह्मचर्य आश्रम) के नियमों का उल्लेख है।
- तृतीय और चतुर्थ अध्याय (गृहस्थ आश्रम): ये अध्याय विवाह के प्रकार, गृहस्थ जीवन के कर्तव्य, पंच महायज्ञ, दान और आजीविका के साधनों पर केंद्रित हैं।
- पंचम अध्याय (भोजन और शुद्धि): इसमें खान-पान के नियम, पवित्रता-अपवित्रता के सिद्धांत और विभिन्न प्रकार की शुद्धि विधियों का वर्णन है।
- षष्ठ अध्याय (वानप्रस्थ और संन्यास): इसमें जीवन के अंतिम दो आश्रमों – वानप्रस्थ (वन में रहना) और संन्यास (त्याग और वैराग्य) के नियम और उनके पालन की विधि बताई गई है।
- सप्तम और अष्टम अध्याय (राजधर्म और न्याय): ये मनुस्मृति के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से हैं, जहाँ राजा के कर्तव्य, शासन प्रणाली, दंड विधान, दीवानी और आपराधिक कानून, गवाही के नियम आदि विस्तार से बताए गए हैं।
- नवम और दशम अध्याय (सामाजिक और आर्थिक नियम): इनमें स्त्री-पुरुष के संबंध, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य और उनके बीच के संबंध, आपातकाल में आजीविका के नियम आदि पर चर्चा की गई है।
- एकादश और द्वादश अध्याय (पाप, प्रायश्चित्त और कर्मफल): अंतिम अध्यायों में विभिन्न प्रकार के पाप, उनके लिए निर्धारित प्रायश्चित्त, कर्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म और मोक्ष के मार्ग का वर्णन है।
यह ग्रंथ उस समय के समाज, उसकी मान्यताओं और नैतिक मूल्यों को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें धर्म (कर्तव्य), अर्थ (धन), काम (इच्छा) और मोक्ष (मुक्ति) के सिद्धांतों को संतुलित करने का प्रयास किया गया है।
मनुस्मृति में ‘धर्म’ और सामाजिक व्यवस्था
मनुस्मृति का केंद्रीय विषय ‘धर्म’ है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा-पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि वह समग्र व्यवस्था है जो समाज को धारण करती है और व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराती है। इसमें व्यक्तिगत आचरण, पारिवारिक संबंध, सामाजिक नियम और राज्य के कानून सभी शामिल हैं। मनुस्मृति में धर्म को चार मुख्य स्तंभों पर आधारित बताया गया है:
- वर्ण व्यवस्था: मनुस्मृति समाज को चार वर्णों – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करती है। प्रत्येक वर्ण के लिए विशिष्ट कर्तव्य (धर्म) और आजीविका के साधन निर्धारित किए गए हैं।
- ब्राह्मण: अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, दान लेना और देना।
- क्षत्रिय: प्रजा की रक्षा, शासन, युद्ध।
- वैश्य: कृषि, पशुपालन, व्यापार।
- शूद्र: अन्य तीन वर्णों की सेवा।
यह विभाजन कार्य और गुणों पर आधारित बताया गया है, हालांकि बाद के काल में यह जन्म आधारित और कठोर हो गया, जिससे कई सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुईं।
- आश्रम व्यवस्था: मनुष्य के जीवन को चार अवस्थाओं में बांटा गया है:
- ब्रह्मचर्य: शिक्षा प्राप्त करना।
- गृहस्थ: विवाह करना और परिवार का पालन-पोषण करना।
- वानप्रस्थ: सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना।
- संन्यास: पूर्ण त्याग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना।
यह व्यवस्था व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करने का एक तरीका थी।
- राजधर्म: राजा के कर्तव्यों और शासन के नियमों का विस्तृत वर्णन है। इसमें न्याय, दंड, कराधान, युद्ध और शांति जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया है। राजा को धर्म का संरक्षक और न्याय का प्रतीक माना गया है।
- व्यक्तिगत धर्म: इसमें सत्य बोलना, अहिंसा, चोरी न करना, इंद्रियों पर नियंत्रण, धैर्य, क्षमा जैसे नैतिक गुणों पर बल दिया गया है, जिन्हें सार्वभौमिक धर्म या ‘मानव धर्म’ कहा जा सकता है।
मनुस्मृति में इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य एक सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना था, जहाँ हर व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत कर सके।
मनुस्मृति की ऐतिहासिक प्रासंगिकता और प्रभाव
मनुस्मृति का भारतीय समाज और कानूनी प्रणाली पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। सदियों तक, यह ग्रंथ हिंदू कानून और सामाजिक मानदंडों के लिए एक संदर्भ बिंदु बना रहा।
- कानूनी और न्यायिक प्रभाव: ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में, जब उन्होंने भारत में कानून बनाना शुरू किया, तो उन्होंने हिंदू व्यक्तिगत कानून के स्रोत के रूप में मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। 1772 में, वारेन हेस्टिंग्स ने घोषणा की कि हिंदुओं पर उनके अपने कानूनों के अनुसार शासन किया जाएगा, और मनुस्मृति को इन ‘हिंदू कानूनों’ के आधार के रूप में देखा गया। इसके कुछ सिद्धांतों, जैसे उत्तराधिकार और विवाह के नियम, को ब्रिटिश अदालतों द्वारा भी मान्यता दी गई।
- सामाजिक और नैतिक प्रभाव: इसने विवाह, परिवार, संपत्ति के अधिकार और व्यक्तिगत आचरण से संबंधित सामाजिक मानदंडों को आकार दिया। इसके द्वारा निर्धारित वर्ण और आश्रम व्यवस्था ने समाज की संरचना को प्रभावित किया, हालांकि समय के साथ इसमें कई विकृतियां भी आईं।
- दार्शनिक और धार्मिक प्रभाव: इसने धर्म, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया और उन्हें हिंदू दर्शन का अभिन्न अंग बना दिया। यह अन्य धर्मशास्त्रों और टीकाओं के लिए भी एक आधार ग्रंथ बना।
- सांस्कृतिक विरासत: मनुस्मृति भारतीय सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें प्राचीन भारतीय समाज, उसके मूल्यों और उसकी कानूनी सोच को समझने में मदद करती है।
यह कहना गलत नहीं होगा कि मनुस्मृति ने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक, नैतिक और कानूनी चिंतन को प्रभावित किया, भले ही आधुनिक युग में इसके कुछ प्रावधानों पर तीव्र बहस और आलोचना होती रही है।
मनुस्मृति से जुड़ी बहसें और आलोचनाएं
जहाँ एक ओर मनुस्मृति को प्राचीन भारतीय समाज के नियमों को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, वहीं दूसरी ओर यह अपने कुछ प्रावधानों के कारण गहन आलोचना का भी विषय रही है। इन आलोचनाओं के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- वर्ण व्यवस्था और जातिगत भेदभाव:
- मनुस्मृति में वर्णों के बीच पदानुक्रम और उनके लिए अलग-अलग नियम निर्धारित किए गए हैं। विशेष रूप से शूद्रों के लिए कठोर नियम और उनके अधिकारों का सीमित होना इसकी सबसे बड़ी आलोचना का कारण है।
- उच्च वर्णों के लिए कम दंड और निम्न वर्णों के लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान भेदभावपूर्ण माना जाता है।
- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जैसे विचारकों ने मनुस्मृति को जातिवाद का मूल स्रोत बताया और इसके प्रावधानों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे भारतीय समाज में असमानता और उत्पीड़न का आधार माना।
- महिलाओं की स्थिति:
- मनुस्मृति में महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहने और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने वाले कई श्लोक हैं (जैसे ‘न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति’ – स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है)।
- संपत्ति के अधिकार, शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी भूमिका को लेकर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिन्हें आधुनिक नारीवादी दृष्टिकोण से प्रतिगामी माना जाता है।
- हालांकि, कुछ श्लोक महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा की बात भी करते हैं, लेकिन समग्र रूप से, आलोचकों का मानना है कि यह ग्रंथ महिलाओं के लिए एक गौण स्थिति निर्धारित करता है।
- दंड विधान की कठोरता:
- मनुस्मृति में कुछ अपराधों के लिए अत्यंत कठोर और शारीरिक दंड का प्रावधान है, जो आधुनिक मानवाधिकार सिद्धांतों के विपरीत हैं।
- वर्ण के आधार पर दंड में भिन्नता भी इसकी न्यायिक प्रणाली को पक्षपातपूर्ण बनाती है।
- अहिंसा का उल्लंघन:
- कुछ आलोचक इसमें पशु बलि और युद्ध संबंधी नियमों को अहिंसा के सिद्धांतों के विपरीत मानते हैं, जबकि हिंदू धर्म में अहिंसा को एक महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य माना जाता है।
इन आलोचनाओं के बावजूद, कुछ विद्वानों का मत है कि मनुस्मृति को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि यह उस समय के समाज की एक तस्वीर प्रस्तुत करती है और इसमें कई नैतिक और प्रशासनिक सिद्धांत भी हैं जो आज भी प्रासंगिक हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसे एक जटिल और बहुआयामी ग्रंथ के रूप में देखना चाहिए, जिसके कुछ अंशों को समकालीन मूल्यों के अनुसार पुनः व्याख्यायित या अस्वीकृत किया जा सकता है।
आधुनिक संदर्भ में मनुस्मृति को कैसे समझें?
मनुस्मृति आज भी भारतीय समाज और उसके इतिहास को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे आधुनिक संदर्भ में समझने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा:
- ऐतिहासिक दस्तावेज़ के रूप में: मनुस्मृति को एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ के रूप में देखा जाना चाहिए जो प्राचीन भारत के सामाजिक, कानूनी और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। यह उस समय की परिस्थितियों और सोच को समझने में मदद करता है। हमें इसे आज के कानूनों या नैतिकता के सीधे पैमाने पर नहीं तोलना चाहिए।
- विकासवादी दृष्टिकोण: भारतीय समाज और कानून हमेशा से स्थिर नहीं रहे हैं; वे समय के साथ विकसित हुए हैं। मनुस्मृति उस विकास प्रक्रिया का एक चरण है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे हिंदू धर्मशास्त्रों की एक विस्तृत श्रृंखला के संदर्भ में देखें, जिसमें अन्य स्मृतियाँ और टीकाएँ भी शामिल हैं जो मनुस्मृति के कुछ प्रावधानों की व्याख्या, संशोधन या आलोचना करती हैं।
- चयनित स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता: आधुनिक भारत एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है जिसका अपना संविधान है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है, जो मनुस्मृति के कुछ प्रावधानों के साथ सीधे टकराव में हैं। इसलिए, मनुस्मृति के उन पहलुओं को जो समानता और न्याय के आधुनिक सिद्धांतों के विपरीत हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- नैतिक और दार्शनिक अंतर्दृष्टि: मनुस्मृति में ऐसे नैतिक सिद्धांत भी हैं जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, आत्म-नियंत्रण, दान और परोपकार। ये सिद्धांत आज भी व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक सद्भाव के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।
- अध्ययन और बहस का विषय: मनुस्मृति एक अकादमिक और बौद्धिक बहस का विषय बनी हुई है। इसका अध्ययन हमें प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन को समझने में मदद करता है। इसके माध्यम से हम उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं जिन्होंने वर्तमान भारतीय समाज को आकार दिया है।
संक्षेप में, मनुस्मृति को एक प्राचीन ग्रंथ के रूप में देखना चाहिए जो हमें इतिहास की एक झलक देता है। हमें इसके सकारात्मक पहलुओं को पहचानना चाहिए और इसके विवादास्पद या प्रतिगामी प्रावधानों को आधुनिक संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों के आलोक में आलोचनात्मक रूप से देखना और अस्वीकार करना चाहिए। इसका उद्देश्य इतिहास से सीखना है, न कि उसे ज्यों का त्यों आज के समाज पर थोपना।
निष्कर्ष
मनुस्मृति को सरल शब्दों में समझना हमें यह दिखाता है कि यह केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय समाज और कानून के विकास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसे सदियों से विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा और परखा गया है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी प्राचीन पाठ को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना कितना आवश्यक है, न कि उसे आज के आधुनिक मूल्यों पर सीधा थोपना। मेरा मानना है कि आज के दौर में, जब हम समानता और न्याय की बात करते हैं, तो ऐसे ग्रंथों का अध्ययन हमें अपने अतीत की जड़ें समझने में मदद करता है, ताकि हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। यह निष्कर्ष हमें केवल मनुस्मृति के बारे में जानकारी नहीं देता, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी देता है: हमें अपनी सोच को हमेशा विकसित करते रहना चाहिए और हर जानकारी को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे आजकल हम डिजिटल युग में फेक न्यूज़ को पहचानते हैं, वैसे ही अतीत के ग्रंथों को भी हमें आज की कसौटी पर परखना होगा, उनकी प्रासंगिकता को समझना होगा। यह हमें सशक्त बनाता है कि हम रूढ़ियों को चुनौती दें और प्रगतिशील समाज के लिए अपने स्वयं के नैतिक मापदंड स्थापित करें। प्रेरणा यही है कि ज्ञान हमें आज़ादी देता है, बशर्ते हम उसका उपयोग सही दिशा में करें। नौकरी छोड़ महिला ने फोन पर शुरू किया ये काम, अब हर महीने कमा रही 10 लाख!
More Articles
यूपी में ‘कूड़ा घोटाला’: हजारों क्विंटल कचरा गायब, 166 होटलों को नगर निगम का नोटिस, बड़ा खुलासा!
आगरा को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस का ‘प्लान-बी’: चौराहों के 100 मीटर दायरे में नो-पार्किंग
भारत-मॉरीशस का बड़ा फैसला: 6000 करोड़ का पैकेज, स्थानीय मुद्रा में होगा कारोबार
झारखंड का वो अनोखा गांव, जहां आबादी है शून्य! आखिर कहां गए सारे लोग?
कृति सैनॉन बॉलीवुड की नई पहचान उनकी सफलता का राज
FAQs
मनुस्मृति क्या है?
मनुस्मृति प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक ग्रंथ है। यह हिंदू धर्मशास्त्रों में से एक है, जिसमें समाज के नियमों, शासन-प्रशासन और व्यक्तिगत आचरण के बारे में विस्तार से बताया गया है।
इसे किसने लिखा था और कब?
परंपरागत रूप से इसे ‘मनु’ नामक ऋषि से जोड़ा जाता है, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में मानव जाति का जनक और पहला कानून निर्माता माना जाता है। हालांकि, विद्वानों का मानना है कि इसे कई सदियों के दौरान विभिन्न लेखकों द्वारा संकलित किया गया था, जिसका रचना काल मोटे तौर पर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा की तीसरी शताब्दी के बीच माना जाता है।
मनुस्मृति में मुख्य रूप से किन विषयों पर जानकारी मिलती है?
इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, चारों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) के कर्तव्य, राजा के नियम, विवाह के प्रकार, उत्तराधिकार, दैनिक अनुष्ठान, प्रायश्चित और न्याय प्रणाली जैसे कई विषयों पर विस्तार से वर्णन है।
क्या मनुस्मृति आज के समय में भी उतनी ही मायने रखती है?
ऐतिहासिक और कानूनी अध्ययन के लिए यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन इसके कई नियम, विशेषकर जाति और लिंग से संबंधित, आधुनिक समाज में भेदभावपूर्ण और पुराने माने जाते हैं। इसलिए, इसे आज के जीवन के लिए सीधा मार्गदर्शक नहीं माना जाता।
मनुस्मृति को लेकर इतने विवाद क्यों हैं?
मनुस्मृति की सबसे बड़ी विवादास्पद बातें वर्ण व्यवस्था में ऊंच-नीच, महिलाओं की निम्न स्थिति और निम्न वर्णों के लिए कठोर दंड से संबंधित प्रावधान हैं। इन्हीं कारणों से इसे आधुनिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ देखा जाता है।
क्या यह सिर्फ एक धार्मिक किताब है?
नहीं, यह केवल एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यह एक ‘धर्मशास्त्र’ है। धर्मशास्त्र में धर्म (सही आचरण) के साथ-साथ सामाजिक, कानूनी और नैतिक नियमों का भी विस्तृत विवरण होता है। यह एक आदर्श समाज के लिए प्राचीन हिंदू परंपराओं पर आधारित नियमों का संग्रह है।
मनुस्मृति का महत्व क्या है?
भारतीय कानूनी इतिहास और सामाजिक संरचना को समझने के लिए मनुस्मृति का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। इसने सदियों तक भारतीय समाज और कानून को प्रभावित किया है, और आज भी इसके प्रभावों को विभिन्न संदर्भों में देखा जा सकता है, भले ही इसके कई प्रावधानों को अब स्वीकार न किया जाता हो।















