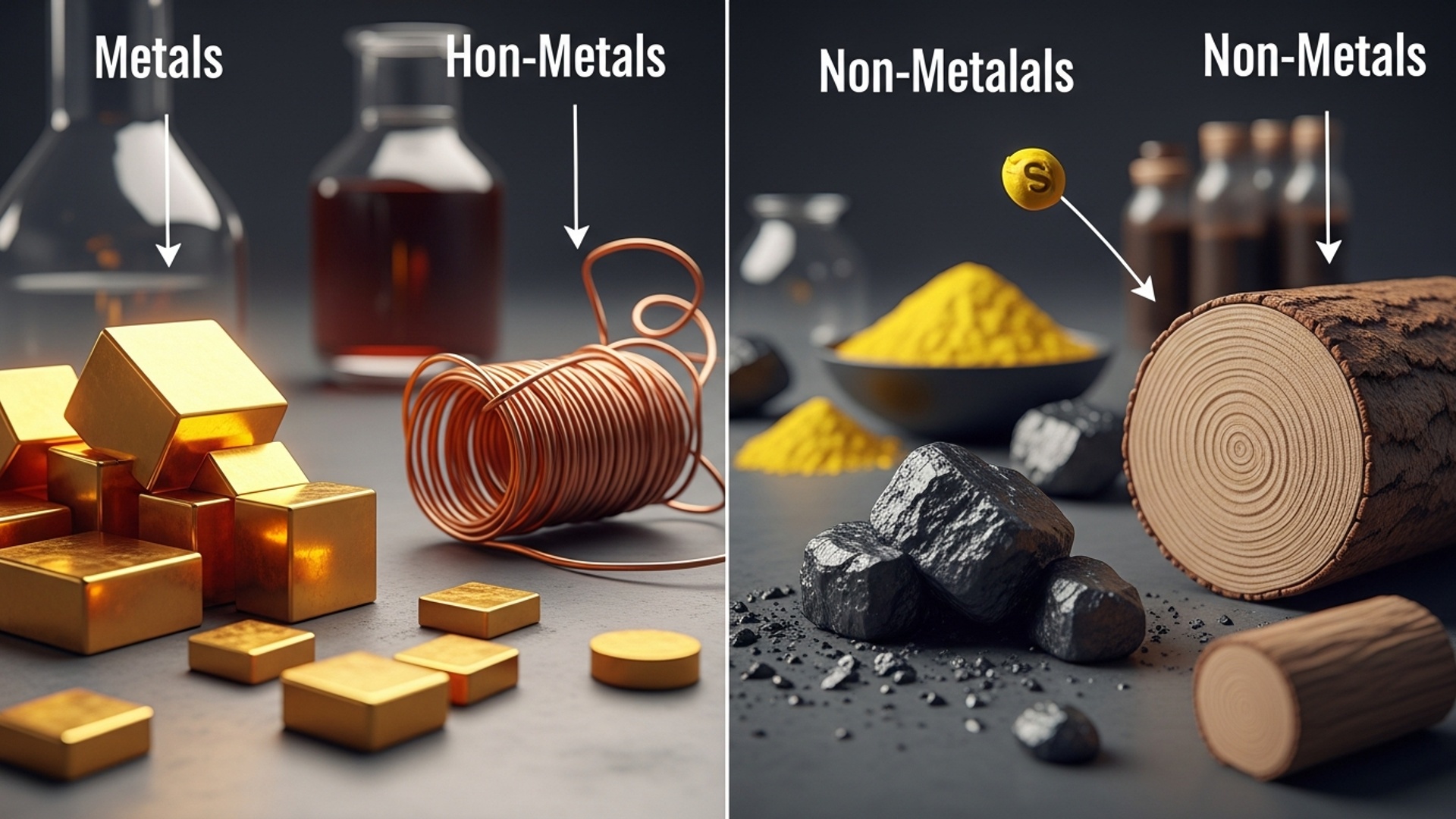बीसवीं सदी की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक, रूसी क्रांति, केवल एक राजनीतिक उथल-पुथल नहीं थी, बल्कि सदियों से दबी हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विसंगतियों का विस्फोटक परिणाम थी। ज़ार निकोलस द्वितीय की निरंकुश सत्ता, भूमिहीन किसानों की दयनीय स्थिति, तीव्र औद्योगीकरण से उपजा श्रमिक वर्ग का असंतोष, और प्रथम विश्व युद्ध की विनाशकारी मार ने एक ऐसे राष्ट्र को कगार पर धकेल दिया था जहाँ परिवर्तन अनिवार्य हो गया। साम्राज्य की अक्षमता और जनता के बढ़ते आक्रोश के बीच, सत्ता के प्रति गहरे अविश्वास ने ‘rusi kranti ke karan’ को जटिल और बहुआयामी बना दिया, जिसने वैश्विक इतिहास की दिशा बदल दी।

ज़ारशाही का निरंकुश और अलोकतांत्रिक शासन
रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक रूस में सदियों से चली आ रही निरंकुश ज़ारशाही व्यवस्था थी। रोमानोव राजवंश के ज़ार पूर्ण सत्तावादी शासक थे, जो ईश्वर प्रदत्त अधिकारों में विश्वास रखते थे। उनके शासन में लोगों को कोई राजनीतिक अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता या प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं था। ज़ार निकोलस द्वितीय, जो क्रांति के समय सत्ता में थे, एक कमजोर शासक थे और अपनी जनता की समस्याओं को समझने या उनका समाधान करने में पूरी तरह अक्षम साबित हुए। वे किसी भी सुधार के खिलाफ थे और अपने सलाहकारों की बात सुनने के बजाय अपनी पत्नी और रहस्यवादी रासपुतिन जैसे अविश्वसनीय व्यक्तियों के प्रभाव में रहते थे। इस दमनकारी शासन के कारण जनता में गहरा असंतोष पनप रहा था, जो अंततः rusi kranti ke karan बना।
- राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव: नागरिकों को संघ बनाने, प्रदर्शन करने या सरकार की आलोचना करने की अनुमति नहीं थी। किसी भी प्रकार के विरोध को क्रूरता से कुचल दिया जाता था।
- प्रशासनिक अक्षमता: ज़ार के अधीन नौकरशाही भ्रष्ट और अक्षम थी, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रही।
- प्रतिनिधित्व का अभाव: ड्यूमा (संसद) जैसी संस्थाएं नाममात्र की थीं और ज़ार की शक्ति को चुनौती देने में असमर्थ थीं।
सामाजिक असमानता और वर्ग संघर्ष
रूसी समाज अत्यधिक असमानता पर आधारित था, जो क्रांति के लिए एक उपजाऊ भूमि साबित हुआ। समाज कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों (जैसे कुलीन वर्ग, पादरी और शाही परिवार) और विशाल गरीब जनता (किसानों और मजदूरों) में बंटा हुआ था। यह गहरी खाई सामाजिक तनाव और वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दे रही थी।
- कुलीन वर्ग और पादरी: इनके पास देश की अधिकांश भूमि और धन था, और ये समाज में सभी प्रमुख पदों पर आसीन थे। इन्हें सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त था।
- किसान (मुजिक): रूस की आबादी का लगभग 80% हिस्सा किसान थे। 1861 में दास प्रथा समाप्त होने के बावजूद, वे अभी भी भूमिहीनता, भारी लगान और गरीबी से जूझ रहे थे। उनके पास खेती के पुराने तरीके थे और वे अक्सर भुखमरी का शिकार होते थे। उनकी भूमि की भूख एक महत्वपूर्ण rusi kranti ke karan थी।
- श्रमिक (सर्वहारा): औद्योगीकरण के कारण शहरों में श्रमिकों का एक नया वर्ग उभर रहा था। ये लोग कारखानों में बेहद खराब परिस्थितियों में, लंबे घंटों तक काम करते थे और उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी। उनके पास यूनियन बनाने या अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी।
यह सामाजिक विभाजन इस हद तक बढ़ गया था कि विभिन्न वर्गों के बीच कोई संवाद नहीं था, जिससे क्रांति की चिंगारी भड़कना स्वाभाविक था।
औद्योगीकरण के प्रभाव और शहरीकरण
19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में सीमित रूप से औद्योगीकरण शुरू हुआ। इसने जहां एक ओर आर्थिक विकास को गति दी, वहीं दूसरी ओर इसने सामाजिक समस्याओं को भी जन्म दिया, जो rusi kranti ke karan में शामिल थीं।
- श्रमिक वर्ग का उदय: कारखानों के विस्तार के साथ, बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी शहरों की ओर पलायन कर गई और श्रमिक बन गई। ये श्रमिक अक्सर भीड़भाड़ वाले, अस्वच्छ शहरी इलाकों में रहते थे और उन्हें भयानक कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था।
- मार्क्सवादी विचारों का प्रसार: कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचार, जो वर्ग संघर्ष और सर्वहारा क्रांति की बात करते थे, इन असंतुष्ट श्रमिकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए। मार्क्सवादी पार्टियों, विशेष रूप से बोल्शेविकों ने इन श्रमिकों को संगठित करना शुरू किया।
- अभाव और असंतोष: शहरीकरण के साथ आवास, भोजन और आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई, जिससे श्रमिकों में गहरा असंतोष फैल गया। हड़तालें और विरोध प्रदर्शन आम बात हो गई थी।
क्रांतिकारी विचारों का प्रसार और राजनीतिक दल
ज़ारशाही के दमनकारी शासन और सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के जवाब में, कई क्रांतिकारी और उदारवादी राजनीतिक दल उभर कर सामने आए, जिन्होंने क्रांति की वैचारिक नींव रखी।
- बोल्शेविक (Bolsheviks): व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, यह एक मार्क्सवादी दल था जो “सर्वहारा वर्ग की तानाशाही” और तत्काल क्रांति के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने में विश्वास रखता था। वे किसानों और मजदूरों के बीच गहरी पैठ बना रहे थे।
- मेंशेविक (Mensheviks): ये भी मार्क्सवादी थे लेकिन उनका मानना था कि रूस को पहले पूंजीवादी चरण से गुजरना होगा और फिर धीरे-धीरे समाजवाद की ओर बढ़ना चाहिए। वे एक बड़े, अधिक समावेशी दल के पक्षधर थे।
- समाजवादी क्रांतिकारी (Socialist Revolutionaries): यह दल मुख्य रूप से किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था और भूमि सुधार तथा कृषि समाजवाद का समर्थन करता था।
- उदारवादी: कुछ उदारवादी समूह भी थे जो संवैधानिक राजतंत्र या संसदीय लोकतंत्र चाहते थे, लेकिन वे क्रांति लाने में उतने कट्टरपंथी नहीं थे।
इन दलों ने गुप्त रूप से काम किया, प्रचार सामग्री वितरित की और जनता को ज़ारशाही के खिलाफ एकजुट करने का प्रयास किया, जिससे rusi kranti ke karan मजबूत होते गए।
प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी
प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी ने ज़ारशाही के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया और रूसी क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। रूस की सेना खराब रूप से सुसज्जित और प्रशिक्षित थी, और युद्ध में उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा।
- सैन्य हारें: पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी के खिलाफ रूस को भारी सैन्य पराजय झेलनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप लाखों रूसी सैनिक मारे गए, घायल हुए या बंदी बना लिए गए।
- आर्थिक दबाव: युद्ध के कारण देश पर जबरदस्त आर्थिक दबाव पड़ा। कारखानों को सैन्य उत्पादन में लगाया गया, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। खाद्य आपूर्ति बाधित हुई, और शहरों में राशन की कमी और कीमतों में भारी वृद्धि हुई।
- जनता का असंतोष: युद्ध के कारण हुए भारी नुकसान, भोजन और ईंधन की कमी ने जनता को हताश कर दिया। ज़ार निकोलस द्वितीय ने स्वयं सेना की कमान संभाली, जिससे उनकी छवि और भी खराब हुई क्योंकि वे युद्ध की विफलताओं के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माने गए।
- राजशाही पर से विश्वास उठना: युद्ध की विफलताएं, ज़ार की अक्षमता और महारानी एलेक्जेंड्रा तथा रासपुतिन का बढ़ता प्रभाव (जो जर्मनी समर्थक माना जाता था) ने राजशाही पर से जनता का रहा-सहा विश्वास भी खत्म कर दिया।
युद्ध की भयावहता ने लोगों को इस बात पर सहमत कर दिया कि बदलाव अब अपरिहार्य है, और यह एक प्रमुख rusi kranti ke karan बन गया।
फरवरी क्रांति (1917) और अंतरिम सरकार की असफलता
1917 की फरवरी में, पेट्रोग्राद (अब सेंट पीटर्सबर्ग) में भोजन की कमी और युद्ध से उपजे असंतोष के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हुईं। सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और उनके साथ शामिल हो गए। इस जनविरोध के कारण ज़ार निकोलस द्वितीय को पद त्यागना पड़ा, जिससे 300 साल पुरानी ज़ारशाही का अंत हो गया।
- ज़ार का त्यागपत्र: सैनिकों और जनता के विद्रोह के बाद, निकोलस द्वितीय ने 15 मार्च 1917 को सिंहासन छोड़ दिया।
- अंतरिम सरकार का गठन: ज़ारशाही के पतन के बाद, एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें उदारवादी और कुछ समाजवादी शामिल थे। इस सरकार का नेतृत्व पहले प्रिंस जॉर्जी ल्वोव और बाद में अलेक्जेंडर केरेन्स्की ने किया।
- अंतरिम सरकार की विफलताएं:
- युद्ध जारी रखना: अंतरिम सरकार ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध जारी रखने का फैसला किया, जिससे जनता का असंतोष और बढ़ गया।
- भूमि सुधार में देरी: किसानों की सबसे बड़ी मांग, भूमि सुधार को अंतरिम सरकार ने टाल दिया, जिससे वे बोल्शेविकों की ओर आकर्षित होने लगे।
- सोवियतों की बढ़ती शक्ति: इसी समय, श्रमिकों और सैनिकों की सोवियतें (परिषदें) भी उभर रही थीं, जो अंतरिम सरकार के साथ सत्ता साझा कर रही थीं (द्वैध शासन)। पेट्रोग्राद सोवियत विशेष रूप से शक्तिशाली थी।
- कानून व्यवस्था बनाए रखने में अक्षमता: सरकार देश में कानून व्यवस्था और बढ़ती अराजकता को नियंत्रित करने में असमर्थ थी।
अंतरिम सरकार की इन विफलताओं ने बोल्शेविकों को सत्ता पर कब्जा करने का अवसर प्रदान किया, और अक्टूबर क्रांति के लिए मंच तैयार किया, जो कि फरवरी क्रांति की विफलता का सीधा परिणाम था और एक महत्वपूर्ण rusi kranti ke karan बन गई।
निष्कर्ष
रूसी क्रांति के मुख्य कारणों को गहराई से समझने के बाद यह स्पष्ट होता है कि सत्ता और जनता के बीच बढ़ता अलगाव, सामाजिक असमानता और आर्थिक बदहाली ही किसी भी बड़े बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार करती है। यह सिर्फ़ इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक है कि जब जनता की आवाज़ को अनसुना किया जाता है, उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं और न्याय की उम्मीद टूट जाती है, तब असंतोष ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। आज भी दुनिया में जब आर्थिक खाई बढ़ती है या सत्ता जनता की आवाज़ को अनसुना करती है, तो तनाव बढ़ता है। मेरी अपनी सीख है कि इतिहास सिर्फ़ पुरानी कहानियाँ नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक सशक्त मार्गदर्शक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी सरकारें समावेशी हों, हर नागरिक की बात सुनें और सबकी खुशहाली के लिए काम करें। एक जागरूक नागरिक के तौर पर, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज और देश की स्थिति पर नज़र रखें और सकारात्मक बदलावों का हिस्सा बनें। आखिरकार, एक खुशहाल और स्थिर समाज तभी बनता है जब हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए, आप खुशहाल जीवन के लिए 5 आसान आदतें जैसे लेख भी पढ़ सकते हैं। आइए, इतिहास से सीखकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाए और सबको समान अवसर मिलें।
More Articles
खुशहाल जीवन के लिए 5 आसान आदतें
MSME को बड़ी पहचान: आगरा में मंत्री, अफसर और उद्यमी मिलकर करेंगे छोटे उद्योगों को ताकतवर बनाने पर मंथन
एसएन मेडिकल कॉलेज में अब दिमाग, लिवर और किडनी की एंजियोप्लास्टी, मरीजों को मिलेगा आधे दाम पर इलाज
यूपी में चौंकाने वाला मामला: दो भाइयों ने मृतक आश्रित कोटे से पाईं दो-दो सरकारी नौकरियां, पेंशन रुकी और जांच शुरू
उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री नंदी का प्रेरणादायक बयान: ‘पहले खोली थी चावल की मिल, आज हूं उद्योग का मंत्री’ – MSME मंथन में गूंजी यह कहानी
FAQs
रूसी क्रांति क्यों हुई, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था?
रूसी क्रांति कई बड़ी वजहों से हुई, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ज़ार निकोलस द्वितीय का निरंकुश और अकुशल शासन था। उनकी नीतियों ने लोगों में भारी असंतोष पैदा कर दिया था, और वह जनता की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह विफल रहे।
क्या गरीब किसानों और मजदूरों की खराब हालत भी क्रांति का एक बड़ा कारण थी?
बिल्कुल! किसानों और मजदूरों की हालत बेहद खराब थी। उनके पास न तो पर्याप्त जमीन थी और न ही उन्हें सही मजदूरी मिलती थी। गरीबी, भुखमरी और काम के अमानवीय हालात ने उन्हें क्रांति के लिए मजबूर कर दिया।
पहले विश्व युद्ध का रूसी क्रांति पर क्या असर पड़ा?
प्रथम विश्व युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था और सेना को बुरी तरह तबाह कर दिया था। सेना को भारी नुकसान हुआ, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई, और महंगाई आसमान छूने लगी। इससे लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया और सरकार के प्रति उनका विश्वास पूरी तरह से उठ गया।
ज़ार के शासन में और क्या कमियां थीं, जिन्होंने क्रांति को जन्म दिया?
ज़ार का शासन अत्यधिक दमनकारी था, जहाँ लोगों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। भ्रष्टाचार चरम पर था और ज़ार अपने सलाहकारों पर अधिक निर्भर थे, बजाय कि जनता की सुनवाई के। उनकी कमजोर नेतृत्व क्षमता और गलत फैसलों ने भी क्रांति की आग को भड़काया।
क्या खाने-पीने की कमी और बढ़ती महंगाई भी एक अहम वजह थी?
हाँ, शहरों में खाने-पीने की चीजों की भारी कमी हो गई थी और कीमतें बेतहाशा बढ़ रही थीं। लोग भूखे मर रहे थे और इस स्थिति ने सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जो अंततः क्रांति में बदल गए।
क्या कोई खास विचार या विचारधारा भी क्रांति के पीछे थी?
हाँ, कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचार रूस में काफी लोकप्रिय हो रहे थे। व्लादिमीर लेनिन जैसे नेताओं ने इन विचारों को फैलाया और लोगों को एकजुट किया, जिससे क्रांति को एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य मिला। इन क्रांतिकारी विचारों ने लोगों को बदलाव के लिए प्रेरित किया।
राजपरिवार से जुड़े किसी विवाद ने भी आग में घी डालने का काम किया था क्या?
हाँ, रासपुतिन नामक एक रहस्यमयी व्यक्ति का ज़ारिना पर अत्यधिक प्रभाव था। उसके गलत कामों और राजपरिवार के मामलों में उसकी दखलअंदाजी ने राजपरिवार की छवि को बुरी तरह खराब किया और जनता का विश्वास और भी कम हो गया, जिससे क्रांति की राह आसान हो गई।