भारत में गरीबी का मापन केवल एक संख्या नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। दशकों से, कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित की जाती रही है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी, लेकिन यह तरीका व्यक्ति की वास्तविक वंचितता को पूरी तरह से नहीं दर्शाता। हाल के वर्षों में, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) ने इस परिदृश्य को बदल दिया है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे कई आयामों को शामिल करता है, जो गरीबी की अधिक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है। 2015-16 से 2019-21 के बीच 13. 5 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, इस नए दृष्टिकोण की सफलता को दर्शाता है। गरीबी को मापने के इन दोनों तरीकों – कैलोरी और बहुआयामी सूचकांक – को समझना भारत की विकास यात्रा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
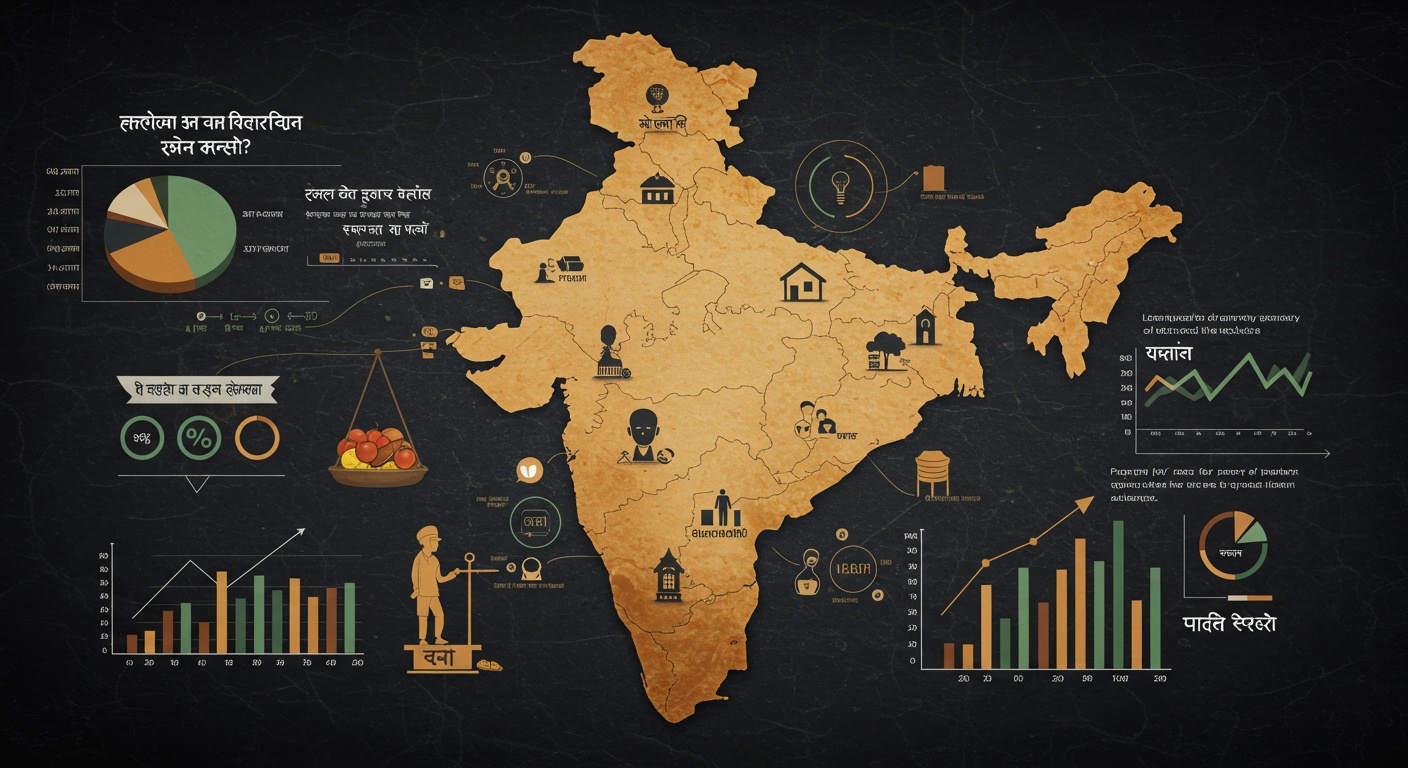
गरीबी मापन का महत्व और उद्देश्य
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में गरीबी एक जटिल चुनौती है। इसे समझना और इसका सटीक मापन करना, प्रभावी नीतियों के निर्माण और संसाधनों के उचित आवंटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरीबी का मापन हमें यह जानने में मदद करता है कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, वे किस प्रकार की अभावग्रस्तता का सामना कर रहे हैं, और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आ रहा है। यह न केवल सरकार के लिए बल्कि शोधकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और आम नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेतक है। गरीबी को मापने के विभिन्न तरीके हैं, और प्रत्येक तरीका अपनी विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन मापन विधियों को समझना, देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कक्षा 9 अर्थशास्त्र में भी गरीबी के इन बुनियादी मापन तरीकों का परिचय दिया जाता है, जो छात्रों को इस गंभीर सामाजिक मुद्दे की प्रारंभिक समझ प्रदान करता है।
कैलोरी आधारित गरीबी रेखा: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
भारत में गरीबी मापने के शुरुआती और सबसे प्रमुख तरीकों में से एक कैलोरी आधारित गरीबी रेखा रही है। इस अवधारणा के अनुसार, एक व्यक्ति को गरीब तब माना जाता है जब वह अपने जीवनयापन के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी का उपभोग करने में असमर्थ होता है।
परिभाषा और गणना
- न्यूनतम पोषण आवश्यकता: यह पद्धति एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम दैनिक कैलोरी आवश्यकताओं को निर्धारित करती है। भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी की आवश्यकता निर्धारित की गई थी। यह अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता को दर्शाता है।
- मौद्रिक मूल्य में रूपांतरण: इन कैलोरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों की लागत का अनुमान लगाकर एक मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है। यह मौद्रिक मूल्य ही गरीबी रेखा कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्राप्त करने के लिए ₹816 प्रति माह की आवश्यकता है, तो यह उस क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा होगी।
- समितियों का योगदान: भारत में विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने इस पद्धति को परिष्कृत किया है:
- वाई. के. अलघ समिति (1979): ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कैलोरी आवश्यकताओं के आधार पर पहली गरीबी रेखा निर्धारित की।
- लकड़वाला समिति (1993): प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट मूल्य सूचकांकों का उपयोग करके गरीबी रेखा का अनुमान लगाया, जिससे राज्य-विशिष्ट गरीबी अनुमान संभव हुए।
- तेंदुलकर समिति (2009): कैलोरी खपत के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को शामिल करके गरीबी रेखा को संशोधित किया, लेकिन अभी भी इसका मुख्य आधार कैलोरी ही था। इसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹27. 20 प्रति व्यक्ति प्रति दिन और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹33. 33 प्रति व्यक्ति प्रति दिन निर्धारित किया।
- रंगराजन समिति (2014): तेंदुलकर समिति के अनुमानों की समीक्षा की और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹32 प्रति व्यक्ति प्रति दिन और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹47 प्रति व्यक्ति प्रति दिन की सिफारिश की।
सीमाएँ और आलोचनाएँ
कैलोरी आधारित गरीबी रेखा की अपनी कई सीमाएँ हैं:
- केवल भोजन पर केंद्रित: यह पद्धति केवल भोजन और कैलोरी पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि गरीबी के कई अन्य महत्वपूर्ण आयामों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास और पीने के पानी की उपेक्षा करती है।
- एकसमान मापदंड: यह विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की विविध आवश्यकताओं और उपभोग पैटर्न को ध्यान में नहीं रखती।
- गुणवत्ता की उपेक्षा: यह केवल कैलोरी की मात्रा पर जोर देती है, न कि उपभोग किए गए भोजन की गुणवत्ता और पोषण मूल्य पर।
- मुद्रास्फीति का प्रभाव: गरीबी रेखा के मौद्रिक मूल्य को मुद्रास्फीति के साथ समायोजित करना एक चुनौती बनी हुई है, जिससे वास्तविक क्रय शक्ति का सही अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है।
- आय बनाम उपभोग: यह उपभोग व्यय पर आधारित है, न कि आय पर, जो अक्सर अनियमित आय वाले लोगों के लिए सटीक नहीं हो सकता।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI): गरीबी की व्यापक समझ
कैलोरी आधारित गरीबी रेखा की सीमाओं को पहचानते हुए, गरीबी को एक अधिक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण से मापने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी आवश्यकता के परिणामस्वरूप बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index – MPI) का विकास हुआ।
MPI क्या है?
MPI एक अंतरराष्ट्रीय उपाय है जो गरीबी को केवल आय या उपभोग के रूप में नहीं, बल्कि कई अभावों के संयोजन के रूप में देखता है जो एक व्यक्ति एक ही समय में अनुभव करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा विकसित किया गया है।
MPI के आयाम और संकेतक
MPI तीन मुख्य आयामों पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक में कई संकेतक शामिल हैं। प्रत्येक आयाम को समान भार (1/3) दिया जाता है, और प्रत्येक संकेतक को उस आयाम के भीतर समान भार दिया जाता है:
| आयाम (भार) | संकेतक (भार) | अभाव की कसौटी (Deprivation Criteria) |
|---|---|---|
| स्वास्थ्य (1/3) | पोषण (1/6) | यदि घर में कोई भी व्यक्ति (विशेषकर बच्चे) कुपोषित है। |
| बाल मृत्यु दर (1/6) | यदि पिछले पांच वर्षों में घर में किसी बच्चे की मृत्यु हुई है। | |
| शिक्षा (1/3) | स्कूली शिक्षा के वर्ष (1/6) | यदि घर का कोई भी सदस्य 6 साल से अधिक की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है। |
| स्कूल में उपस्थिति (1/6) | यदि स्कूल जाने की उम्र का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। | |
| जीवन स्तर (1/3) | खाना पकाने का ईंधन (1/18) | यदि घर मुख्य रूप से गोबर, लकड़ी या फसल अवशेषों से खाना पकाता है। |
| स्वच्छता (1/18) | यदि घर में बेहतर शौचालय नहीं है या वह साझा है। | |
| पीने का पानी (1/18) | यदि घर के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है या इसे प्राप्त करने में 30 मिनट से अधिक लगते हैं। | |
| बिजली (1/18) | यदि घर में बिजली नहीं है। | |
| आवास (1/18) | यदि घर मिट्टी, घास, या अन्य खराब गुणवत्ता वाली सामग्री से बना है। | |
| संपत्ति (1/18) | यदि घर में रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, जानवर, साइकिल, मोटरसाइकिल या रेफ्रिजरेटर में से कोई भी संपत्ति नहीं है या केवल एक है। |
MPI की गणना कैसे होती है?
- प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा अनुभव किए गए अभावों के आधार पर एक ‘अभाव स्कोर’ (Deprivation Score) दिया जाता है।
- यदि किसी व्यक्ति का अभाव स्कोर कुल भारित संकेतकों के 33. 3% या अधिक तक पहुँच जाता है, तो उसे बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है।
- MPI गरीबी में रहने वाले लोगों के अनुपात (घटना) और उन अभावों की औसत संख्या या तीव्रता (तीव्रता) का एक उत्पाद है जो गरीब लोग एक साथ अनुभव करते हैं।
भारत में MPI का उपयोग
भारत में, नीति आयोग (NITI Aayog) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) के साथ मिलकर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National MPI) जारी करता है। यह सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों पर आधारित है और विभिन्न राज्यों और जिलों में गरीबी के स्तर को समझने में मदद करता है। यह सरकारों को लक्षित हस्तक्षेपों और नीतियों को डिजाइन करने में सहायता करता है ताकि सबसे वंचित आबादी तक पहुँच बनाई जा सके। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में पोषण और स्वच्छता में उच्च अभाव देखा जाता है, तो वहाँ इन क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
कैलोरी आधारित गरीबी रेखा बनाम बहुआयामी गरीबी सूचकांक
इन दोनों मापन प्रणालियों की तुलना से उनकी शक्तियों और कमजोरियों को समझना आसान हो जाता है:
| विशेषता | कैलोरी आधारित गरीबी रेखा | बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) |
|---|---|---|
| आधार | न्यूनतम कैलोरी उपभोग के लिए आवश्यक मौद्रिक व्यय। | स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में एक साथ कई अभाव। |
| दायरा | संकीर्ण; मुख्य रूप से भोजन और पोषण पर केंद्रित। | व्यापक; मानव विकास के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है। |
| माप की इकाई | प्रति व्यक्ति प्रति दिन/माह का मौद्रिक मूल्य। | अभावों की संख्या और तीव्रता। |
| नीतिगत निहितार्थ | आय सहायता या खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों पर ध्यान। | लक्षित, बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा) की पहचान। |
| जटिलता | सरल और समझने में आसान। | अधिक जटिल, लेकिन गरीबी की अधिक सटीक तस्वीर प्रस्तुत करता है। |
| ऐतिहासिक उपयोग | भारत में लंबे समय से उपयोग में है। | हाल के वर्षों में अधिक प्रमुखता प्राप्त की है। |
MPI को अक्सर कैलोरी आधारित गरीबी रेखा से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह गरीबी की एक अधिक वास्तविक और मानवीय तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, बल्कि यह अवसरों और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी भी है। यह नीति निर्माताओं को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जिससे अधिक प्रभावी और लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बनाए जा सकें।
भारत में गरीबी मापन की चुनौतियाँ और भविष्य
भारत में गरीबी का मापन एक निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र है। यद्यपि कैलोरी आधारित और बहुआयामी सूचकांकों ने महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं:
- डेटा की उपलब्धता और सटीकता: बड़े पैमाने पर, विश्वसनीय और अद्यतन डेटा एकत्र करना एक बड़ी चुनौती है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
- शहरीकरण और प्रवासन: शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या और ग्रामीण-शहरी प्रवासन गरीबी के स्वरूप को बदल रहा है, जिसके लिए नए मापन दृष्टिकोणों की आवश्यकता है।
- अदृश्य गरीबी: कुछ प्रकार की गरीबी, जैसे कि छिपी हुई बेरोजगारी या मौसमी गरीबी, को पारंपरिक मापन विधियों से पकड़ना मुश्किल होता है।
- सामाजिक-सांस्कृतिक कारक: गरीबी केवल आर्थिक नहीं होती; यह अक्सर सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और असुरक्षा से भी जुड़ी होती है, जिन्हें मात्रात्मक रूप से मापना कठिन होता है।
- नीतिगत सामंजस्य: विभिन्न मापन पद्धतियों से प्राप्त आंकड़ों को नीतियों में प्रभावी ढंग से एकीकृत करना और यह सुनिश्चित करना कि वे जमीनी स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालें, एक जटिल कार्य है।
भविष्य में, गरीबी मापन में और अधिक परिष्करण देखने को मिल सकता है, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग (जैसे उपग्रह इमेजरी और बिग डेटा), अधिक सूक्ष्म सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का समावेश, और विभिन्न मापन प्रणालियों के बीच बेहतर सामंजस्य शामिल है। लक्ष्य हमेशा यही रहेगा कि गरीबी की एक स्पष्ट, सटीक और कार्रवाई योग्य तस्वीर प्राप्त की जाए ताकि भारत से गरीबी को जड़ से खत्म करने के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। यह विशेष रूप से कक्षा 9 अर्थशास्त्र और उच्चतर अध्ययन के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे इन जटिलताओं को समझें ताकि वे भविष्य में बेहतर समाधानों में योगदान कर सकें।
निष्कर्ष
भारत में गरीबी का मापन केवल कैलोरी या आय तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब यह शिक्षा, स्वास्थ्य, और जीवन-स्तर जैसे बहुआयामी पहलुओं को भी समाहित करता है। यह बदलाव दर्शाता है कि हम गरीबी को अब सिर्फ ‘पेट भरने’ की समस्या नहीं, बल्कि ‘सम्मान से जीने’ के अधिकार के रूप में देख रहे हैं। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी दर्शाया है कि भारत बहुआयामी गरीबी घटाने में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, जो इस व्यापक दृष्टिकोण की सफलता का प्रमाण है। इस जटिल मापन को समझना हमें गरीबी के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है। व्यक्तिगत रूप से, मैं हमेशा यह मानता रहा हूँ कि ज्ञान ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। यदि हम गरीबी के वास्तविक स्वरूप और उसके मापन को समझेंगे, तो बेहतर नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने में अपना योगदान दे पाएंगे। आप भी अपने आस-पास के लोगों को शिक्षा और कौशल विकास के महत्व के प्रति जागरूक करके इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि मानव पूंजी का विकास ही स्थायी समाधान है। यह केवल सरकारी नीतियों का विषय नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए, एक ऐसे भारत के निर्माण में अपना योगदान दें जहाँ हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले।
More Articles
गरीबी के बहुआयामी रूप और प्रमुख कारण समझें
गरीबी रेखा को समझें भारत में निर्धनता का आकलन कैसे होता है
भारत में गरीबी के कारण और इसे दूर करने के प्रभावी उपाय
मानव पूंजी का महत्व और भारत में रोजगार के अवसर
कैसे बनें अर्थव्यवस्था की संपत्ति? जानें शिक्षा और कौशल विकास का महत्व
FAQs
भारत में गरीबी का मापन किन प्रमुख तरीकों से किया जाता है?
भारत में गरीबी मापने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके अपनाए जाते हैं: पहला, उपभोग व्यय पर आधारित गरीबी रेखा (जो कैलोरी मानदंड से जुड़ी थी), और दूसरा, हाल ही में अपनाया गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)।
भारत में गरीबी रेखा क्या है और इसका कैलोरी मानदंड से क्या संबंध रहा है?
गरीबी रेखा वह न्यूनतम आय या उपभोग स्तर है जो किसी व्यक्ति को बुनियादी आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, आवास) को पूरा करने के लिए आवश्यक है। पहले, इसे मुख्य रूप से कैलोरी मानदंड (ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) के आधार पर निर्धारित किया जाता था, यानी जो व्यक्ति इतनी कैलोरी उपभोग करने में सक्षम नहीं थे, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना जाता था।
कैलोरी आधारित गरीबी मापन पद्धति की मुख्य कमियाँ क्या थीं?
कैलोरी आधारित मापन की प्रमुख कमी यह थी कि यह केवल भोजन उपभोग पर केंद्रित था और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल, स्वच्छता और आवास जैसी अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को अनदेखा करता था। यह गरीबी की जटिल प्रकृति को पूरी तरह से नहीं दर्शाता था।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) से आप क्या समझते हैं और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) गरीबी को केवल आय या कैलोरी के बजाय कई आयामों में मापता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे प्रमुख संकेतकों पर व्यक्तियों की अभावग्रस्तता को देखता है। यह गरीबी की अधिक व्यापक और सटीक तस्वीर प्रस्तुत करता है।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में गरीबी को मापने के लिए किन प्रमुख आयामों और संकेतकों का उपयोग किया जाता है?
MPI में तीन प्रमुख आयाम शामिल हैं: 1. स्वास्थ्य (पोषण और बाल मृत्यु दर), 2. शिक्षा (स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति), और 3. जीवन स्तर (खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और संपत्ति)। यदि कोई व्यक्ति इन संकेतकों में से एक तिहाई या अधिक में अभावग्रस्त पाया जाता है, तो उसे बहुआयामी गरीब माना जाता है।
कैलोरी आधारित गरीबी मापन और बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के बीच मुख्य अंतर क्या है?
कैलोरी आधारित मापन मुख्य रूप से भोजन उपभोग और आय पर केंद्रित था, जबकि MPI गरीबी को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के विभिन्न पहलू शामिल हैं। MPI गरीबी की गंभीरता और इसके विभिन्न रूपों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, जबकि कैलोरी मापन एक संकीर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता था।
भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए कौन-कौन सी प्रमुख समितियाँ गठित की गई हैं?
भारत में गरीबी के आकलन के लिए कई समितियाँ गठित की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं: वाई. के. अलग समिति (1979), सुरेश तेंदुलकर समिति (2009), और सी. रंगराजन समिति (2014)। वर्तमान में, नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) रिपोर्ट जारी की जाती है।
















