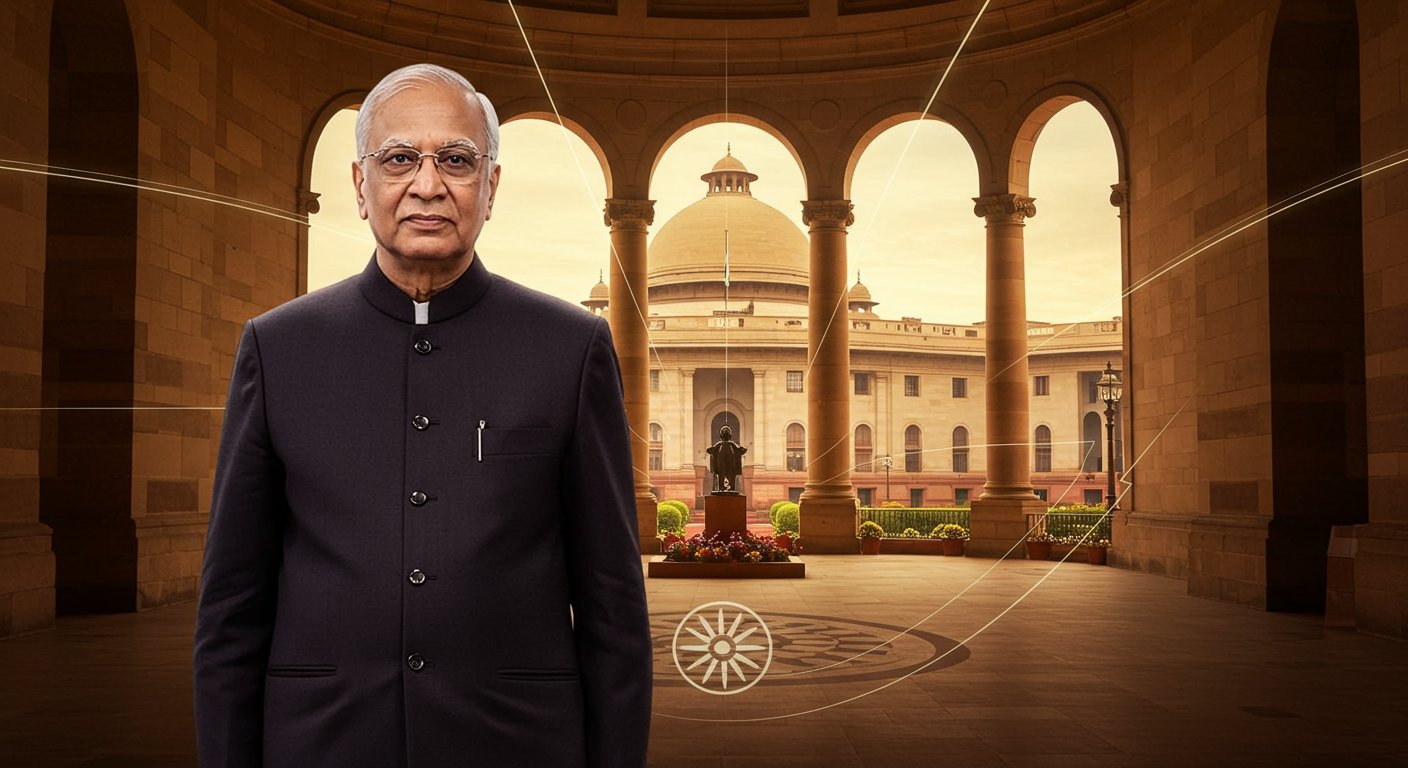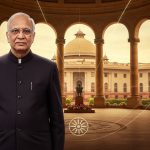आज के तीव्र गति वाले युग में, जहाँ मानसिक शांति और सामाजिक सामंजस्य की तलाश एक वैश्विक चुनौती बन गई है, प्राचीन ज्ञान स्रोत हमें राह दिखाते हैं। मनुस्मृति, जिसे अक्सर उसके कानूनी पहलुओं के लिए जाना जाता है, ‘परम कल्याण’ प्राप्त करने के लिए छह आवश्यक कर्मों (षट्कर्म) का विस्तृत वर्णन करती है। ये कर्म केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुशासन, नैतिक आचरण और आत्म-विकास के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक हैं। आधुनिक समय में जब नैतिकता और मानसिक स्वास्थ्य पर बहसें तीव्र हैं, ये सिद्धांत आत्म-नियंत्रण, ज्ञानार्जन और परोपकारिता के माध्यम से एक संतुलित जीवन की नींव रखते हैं, जो वर्तमान डिजिटल भटकाव और सामाजिक तनावों के बीच विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।

ज्ञानार्जन और आत्म-चिंतन: परम सत्य की खोज (अध्ययन)
मनुस्मृति, भारतीय चिंतन परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो समाज और व्यक्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसमें बताए गए छह आवश्यक कर्मों में से पहला है ‘अध्ययन’। आमतौर पर इसे वेदों और शास्त्रों के अध्ययन से जोड़ा जाता है, लेकिन परम कल्याण के संदर्भ में इसका अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। यह केवल धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना नहीं, बल्कि ज्ञान की निरंतर खोज, आत्म-चिंतन और स्वयं को बेहतर समझने की प्रक्रिया है।
- निरंतर सीखना: आज के दौर में अध्ययन का अर्थ केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। यह जीवनभर सीखने की प्रक्रिया है – नई भाषाओं को सीखना, कौशल विकसित करना, विभिन्न संस्कृतियों को समझना, या यहां तक कि अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करना। यह हमें बदलते समय के साथ अनुकूलन करने और नए अवसरों को पहचानने में मदद करता है।
- आत्म-चिंतन: अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू आत्म-चिंतन है। इसका अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का विश्लेषण करना। यह हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने में मदद करता है, जिससे हम व्यक्तिगत विकास की दिशा में काम कर सकते हैं।
- सत्य की खोज: मनुस्मृति में अध्ययन का मूल उद्देश्य सत्य की खोज करना है। यह सत्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी निहित है। ध्यान, योग और आत्म-मंथन के माध्यम से हम अपने अंतरतम सत्य से जुड़ सकते हैं, जिससे हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है।
वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग: कल्पना कीजिए एक उद्यमी जो अपने क्षेत्र के नवीनतम रुझानों का लगातार अध्ययन करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और आत्म-चिंतन के माध्यम से अपनी नेतृत्व क्षमता में सुधार करता है। यह निरंतर अध्ययन और आत्म-चिंतन ही उसे बाजार में टिके रहने और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। यह मनुस्मृति के ‘अध्ययन’ कर्म का एक आधुनिक और व्यावहारिक उदाहरण है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर कल्याण की ओर ले जाता है।
विद्या-दान और मार्गदर्शन: ज्ञान बांटने का पुनीत कार्य (अध्यापन)
मनुस्मृति द्वारा बताए गए छह आवश्यक कर्मों में दूसरा महत्वपूर्ण कर्म है ‘अध्यापन’, जिसका अर्थ है ज्ञान का दान या दूसरों को शिक्षित करना। यह केवल औपचारिक शिक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अपने अनुभव, अंतर्दृष्टि और कौशल को दूसरों के साथ साझा करना भी शामिल है, ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें।
- ज्ञान का प्रसार: अध्यापन का सबसे सीधा अर्थ है दूसरों को पढ़ाना। यह स्कूल, कॉलेज में हो सकता है, या अनौपचारिक रूप से घर या समुदाय में हो सकता है। जब हम अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम न केवल उन्हें सशक्त बनाते हैं, बल्कि हम अपने स्वयं के ज्ञान को भी सुदृढ़ करते हैं।
- मार्गदर्शन और सलाह: अध्यापन में केवल तथ्यों को बताना ही नहीं, बल्कि दूसरों को सही मार्ग पर मार्गदर्शन करना और उन्हें सलाह देना भी शामिल है। एक गुरु, संरक्षक या यहां तक कि एक अनुभवी सहकर्मी भी इस भूमिका को निभा सकता है। यह उन्हें चुनौतियों का सामना करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है।
- क्षमताओं का विकास: दूसरों को पढ़ाना या मार्गदर्शन करना उन्हें अपनी क्षमता का एहसास करने और उसे विकसित करने में मदद करता है। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है और उन्हें समाज में सकारात्मक योगदान करने के लिए प्रेरित करता है।
वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग: एक अनुभवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने जूनियर डेवलपर्स को न केवल कोड सिखाता है, बल्कि उन्हें समस्या-समाधान के तरीके भी बताता है और उनके करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह व्यक्ति मनुस्मृति के ‘अध्यापन’ कर्म का पालन कर रहा है। उसके इस प्रयास से न केवल जूनियर डेवलपर्स का विकास होता है, बल्कि टीम की समग्र उत्पादकता भी बढ़ती है, जिससे सामूहिक कल्याण होता है। इसी तरह, एक स्वयंसेवक जो वंचित बच्चों को पढ़ाता है या एक समुदाय का सदस्य जो अपने पड़ोसियों को बागवानी के तरीके सिखाता है, वे सभी इस कर्म का पालन कर रहे हैं।
आत्म-संयम और समर्पण: आंतरिक अग्नि का पोषण (यजन)
मनुस्मृति के अनुसार, ‘यजन’ तीसरा आवश्यक कर्म है। पारंपरिक रूप से, यजन का अर्थ अग्नि में आहुति देकर देवताओं की पूजा करना या यज्ञ करना है। हालांकि, परम कल्याण के आधुनिक संदर्भ में, इसे आंतरिक अनुशासन, आत्म-संयम और अपने उच्च उद्देश्यों के प्रति समर्पण के रूप में समझा जा सकता है। यह बाहरी अनुष्ठानों से परे जाकर अपनी आंतरिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का प्रतीक है।
- इच्छाओं पर नियंत्रण: यजन का एक महत्वपूर्ण पहलू अपनी भौतिकवादी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। यह हमें क्षणिक सुखों से ऊपर उठकर दीर्घकालिक लक्ष्यों और नैतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह आत्म-संयम हमें व्यसनों और नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचाता है।
- अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण: यजन का अर्थ है अपने निर्धारित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना। चाहे वह पारिवारिक कर्तव्य हो, व्यावसायिक जिम्मेदारी हो या सामाजिक योगदान हो, उन्हें पूरी निष्ठा से करना ही एक प्रकार का आंतरिक यज्ञ है।
- आंतरिक शुद्धिकरण: यह कर्म हमें अपने भीतर की नकारात्मकताओं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार को त्यागने के लिए प्रेरित करता है। इन आंतरिक बाधाओं को दूर करना एक प्रकार का ‘आत्म-यज्ञ’ है, जो हमें मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धता प्रदान करता है।
वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग: एक खिलाड़ी जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण लेता है, अपनी पसंदीदा चीजों का त्याग करता है और हर दिन अनुशासन का पालन करता है, वह ‘यजन’ के इस कर्म का पालन कर रहा है। उसकी सफलता केवल बाहरी जीत नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। इसी तरह, एक शोधकर्ता जो वर्षों तक एक जटिल समस्या को हल करने के लिए अथक प्रयास करता है, या एक कलाकार जो अपनी कला को निखारने के लिए आत्म-संयम और एकाग्रता का अभ्यास करता है, वे सभी ‘यजन’ के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार रहे हैं। यह आंतरिक अग्नि का पोषण है जो उन्हें उनके लक्ष्यों तक पहुंचाता है।
प्रेरणा और सामूहिकता का सूत्र: दूसरों को सही राह दिखाना (याजन)
मनुस्मृति के छह कर्मों में ‘याजन’ चौथा महत्वपूर्ण कर्म है। यदि ‘यजन’ स्वयं के लिए यज्ञ करना है, तो ‘याजन’ दूसरों को यज्ञ करने या शुभ कर्मों में प्रवृत्त करने का अर्थ रखता है। आधुनिक और व्यापक संदर्भ में, इसका अर्थ है दूसरों को अच्छे और नैतिक कार्यों के लिए प्रेरित करना, उन्हें सही दिशा दिखाना और सामूहिक कल्याण के लिए प्रेरित करना। यह एक प्रकार का नेतृत्व है जो सकारात्मक बदलाव लाता है।
- उदाहरण स्थापित करना: ‘याजन’ का सबसे प्रभावी तरीका स्वयं एक उदाहरण स्थापित करना है। जब लोग आपको ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दयालुता के साथ कार्य करते देखते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और उन्हीं मूल्यों को अपनाने का प्रयास करते हैं।
- सकारात्मक प्रभाव डालना: इसमें दूसरों को उनके कर्तव्यों का पालन करने, नैतिक रूप से कार्य करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। यह व्यक्तिगत सलाह, सार्वजनिक भाषण या सामुदायिक पहलों के माध्यम से हो सकता है।
- सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना: ‘याजन’ का अर्थ है लोगों को एक साथ लाना और उन्हें एक सामान्य, अच्छे उद्देश्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना। यह सामुदायिक परियोजनाओं, सामाजिक आंदोलनों या परोपकारी गतिविधियों का आयोजन करके किया जा सकता है।
वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग: एक सामुदायिक नेता जो अपने पड़ोसियों को सफाई अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, या एक टीम लीडर जो अपनी टीम के सदस्यों को चुनौतीपूर्ण परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, वे ‘याजन’ के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। वे न केवल स्वयं कार्य कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी उस कार्य में शामिल होने और योगदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह मनुस्मृति की शिक्षा का एक शक्तिशाली पहलू है जो व्यक्तिगत प्रयास से परे जाकर सामूहिक शक्ति का उपयोग कर समाज को बेहतर बनाता है। एक शिक्षक जो अपने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है, या एक माता-पिता जो अपने बच्चों को ईमानदारी का महत्व सिखाता है, वे सभी इस कर्म का पालन कर रहे हैं।
निस्वार्थ भाव से देना: उदारता और सेवा का मार्ग (दान)
मनुस्मृति द्वारा बताए गए छह आवश्यक कर्मों में पांचवां ‘दान’ है। दान का अर्थ केवल धन का दान करना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना है। यह भौतिक वस्तुओं के साथ-साथ समय, ज्ञान, कौशल, प्रेम और दया का दान भी हो सकता है। दान का मूल उद्देश्य सामाजिक समरसता और कल्याण को बढ़ावा देना है।
- भौतिक दान: इसमें जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, आश्रय या धन प्रदान करना शामिल है। यह एक प्राचीन परंपरा है जो समाज के वंचित वर्गों को सहारा देती है और आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करती है।
- समय और कौशल का दान: दान केवल धन तक सीमित नहीं है। अपने समय का दान करना (जैसे स्वयंसेवा करना) या अपने विशेष कौशल (जैसे चिकित्सा सहायता, कानूनी सलाह, शिक्षण) का दान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सीधे तौर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करता है।
- प्रेम और दया का दान: दान का सबसे सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली रूप प्रेम, दया, करुणा और सहानुभूति का दान है। किसी को सुनना, सांत्वना देना, या सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाना भी एक प्रकार का दान है जो किसी के दिन को रोशन कर सकता है।
वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग: एक डॉक्टर जो अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर ग्रामीण इलाकों में मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित करता है, वह मनुस्मृति के ‘दान’ कर्म का पालन कर रहा है। वह न केवल अपने ज्ञान और कौशल का दान कर रहा है, बल्कि अपना अमूल्य समय भी दे रहा है। इसी तरह, एक व्यक्ति जो नियमित रूप से एक वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों के साथ समय बिताता है, या एक छात्र जो अपने पड़ोस के बच्चों को पढ़ाता है, वे सभी निस्वार्थ भाव से ‘दान’ कर रहे हैं। यह कर्म हमें अपनी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठकर एक बड़े समुदाय का हिस्सा बनने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें कृतज्ञता और संतुष्टि की गहरी भावना प्रदान करता है।
कृतज्ञता और विवेकपूर्ण स्वीकार्यता: प्राप्तियों का सम्मान (प्रतिग्रह)
मनुस्मृति द्वारा वर्णित छह आवश्यक कर्मों में अंतिम और अक्सर गलत समझा जाने वाला कर्म है ‘प्रतिग्रह’। पारंपरिक रूप से, इसका अर्थ है योग्य व्यक्तियों से दान या उपहार स्वीकार करना। हालांकि, परम कल्याण के व्यापक संदर्भ में, ‘प्रतिग्रह’ का अर्थ है प्राप्त होने वाली हर चीज़ को कृतज्ञता और विवेकपूर्ण तरीके से स्वीकार करना, चाहे वह भौतिक वस्तु हो, ज्ञान हो, अवसर हो या दूसरों का सहयोग हो। इसमें प्राप्त की गई चीज़ों की जिम्मेदारी को समझना भी शामिल है।
- कृतज्ञता का भाव: प्रतिग्रह का मूल मंत्र कृतज्ञता है। जो कुछ भी हमें मिलता है – प्रकृति से, समाज से, परिवार से, या किसी व्यक्ति से – उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। यह हमें विनम्र बनाता है और जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को पहचानने में मदद करता है।
- विवेकपूर्ण स्वीकार्यता: ‘प्रतिग्रह’ का अर्थ यह भी है कि हमें हर चीज़ को बिना सोचे-समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि क्या हमारे लिए, समाज के लिए और हमारे मूल्यों के लिए सही है। गलत तरीकों से प्राप्त लाभ या ऐसी चीज़ें जो हमें नैतिक रूप से भ्रष्ट करती हैं, उनसे बचना चाहिए।
- जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करना: जब हम कुछ प्राप्त करते हैं, तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। उदाहरण के लिए, यदि हमें ज्ञान मिलता है, तो उसे सही ढंग से उपयोग करने की जिम्मेदारी है। यदि हमें धन मिलता है, तो उसे समाज के कल्याण के लिए उपयोग करने की जिम्मेदारी है। यह मनुस्मृति का एक महत्वपूर्ण संदेश है।
वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग: एक छात्र जो अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान का उपयोग समाज के भले के लिए करता है, वह ‘प्रतिग्रह’ के इस कर्म का पालन कर रहा है। वह न केवल ज्ञान को स्वीकार करता है, बल्कि उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और उसे जिम्मेदारी से उपयोग करता है। इसी प्रकार, एक व्यक्ति जिसे समुदाय से समर्थन मिलता है और वह उस समर्थन का उपयोग अपनी और दूसरों की मदद करने के लिए करता है, वह भी ‘प्रतिग्रह’ का पालन कर रहा है। यह कर्म हमें सिखाता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और हमें दूसरों से प्राप्त होने वाले सहयोग और संसाधनों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें संजोना चाहिए और उनका उपयोग सकारात्मक रूप से करना चाहिए। यह एक संतुलित जीवन जीने और समाज में अपनी भूमिका को समझने का मार्ग है।
निष्कर्ष
मनुस्मृति द्वारा बताए गए ये 6 आवश्यक कर्म केवल प्राचीन नियम नहीं, बल्कि परम कल्याण की ओर ले जाने वाले शाश्वत सिद्धांत हैं। आज की आधुनिक, भागदौड़ भरी जीवनशैली में भी इनकी प्रासंगिकता उतनी ही है जितनी सदियों पहले थी। मेरा अपना अनुभव बताता है कि जब मैंने अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी और आत्म-संयम जैसे गुणों को प्राथमिकता देनी शुरू की, तो भीतर एक अद्भुत शांति और स्पष्टता का अनुभव हुआ। यह सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सौहार्द का भी सीधा मार्ग है। इन कर्मों को अपने जीवन में उतारने की शुरुआत छोटे कदमों से करें। उदाहरण के लिए, एक सप्ताह के लिए किसी एक कर्म – जैसे ‘सत्य’ या ‘अस्तेय’ (अचोरी) – को पूर्ण निष्ठा से अभ्यास करने का संकल्प लें। आप देखेंगे कि कैसे यह एक छोटा सा बदलाव आपके व्यवहार और दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। याद रखें, परम कल्याण कोई दूर का गंतव्य नहीं, बल्कि इन सिद्धांतों को अपनाने से प्रत्येक पल में प्राप्त होने वाली अवस्था है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है जो आपको स्वयं से और संसार से बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद करेगी।
More Articles
अस्तेय क्या है मनुस्मृति के अनुसार
दैनिक जीवन में पवित्रता कैसे बनाए रखें मनुस्मृति से सीखें
सदाचार का महत्व: मनुस्मृति से सीखें उत्तम जीवन जीने के सूत्र
आत्मिक शुद्धिकरण का प्राचीन ज्ञान मनुस्मृति से सीखें
मनुस्मृति में क्षमा का महत्व
FAQs
परम कल्याण के लिए मनुस्मृति में बताए गए 6 आवश्यक कर्म कौन-कौन से हैं?
मनुस्मृति के अनुसार परम कल्याण की प्राप्ति के लिए 6 आवश्यक कर्म हैं: अध्ययन (वेदों का अध्ययन), अध्यापन (वेदों का शिक्षण), यजन (स्वयं के लिए यज्ञ करना), याजन (दूसरों के लिए यज्ञ करवाना), दान (दान देना), और प्रतिग्रह (योग्य व्यक्ति से दान स्वीकार करना)।
मनुस्मृति में इन 6 कर्मों को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है?
इन कर्मों को अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि ये व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। ये कर्म न केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि सामाजिक व्यवस्था और नैतिक आचरण के लिए भी आधारभूत माने गए हैं।
‘अध्ययन’ और ‘अध्यापन’ से क्या अभिप्राय है?
‘अध्ययन’ का अर्थ है स्वयं वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त करना। वहीं, ‘अध्यापन’ का अर्थ है उस प्राप्त ज्ञान को दूसरों को सिखाना और उसका प्रचार-प्रसार करना। ये दोनों ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक हैं।
‘यजन’ और ‘याजन’ में क्या अंतर है?
‘यजन’ का अर्थ है स्वयं के लिए यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना। इसके विपरीत, ‘याजन’ का अर्थ है दूसरों के लिए यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान करवाना। दोनों ही समाज में धार्मिकता और पवित्रता को बढ़ावा देते हैं।
‘दान’ और ‘प्रतिग्रह’ का परम कल्याण से क्या संबंध है?
‘दान’ का अर्थ है निस्वार्थ भाव से योग्य और जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और सामाजिक संतुलन बना रहता है। ‘प्रतिग्रह’ का अर्थ है योग्य व्यक्ति से, धर्म सम्मत तरीके से, दान या उपहार स्वीकार करना। ये दोनों ही क्रियाएं समाज में संसाधनों के उचित वितरण और पारस्परिक सहयोग को दर्शाती हैं, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक और लौकिक दोनों तरह के कल्याण की ओर ले जाती हैं।
क्या ये सभी 6 कर्म समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक माने गए हैं या इनका कोई विशेष संदर्भ है?
मनुस्मृति में इन छह कर्मों को विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए विहित किया गया है, जिन्हें समाज में ज्ञान और धर्म के वाहक तथा संरक्षक के रूप में देखा जाता था। हालाँकि, इनके मूल सिद्धांत जैसे ज्ञानार्जन, परोपकार, धार्मिकता और नैतिक आचरण सभी वर्गों के लिए प्रासंगिक हैं, भले ही उनके कर्मों का स्वरूप और तरीका भिन्न हो।
आधुनिक युग में मनुस्मृति के इन 6 कर्मों का क्या महत्व है और इन्हें कैसे समझा जा सकता है?
आधुनिक युग में भी इन कर्मों का महत्व बना हुआ है, यद्यपि इन्हें व्यापक संदर्भ में समझा जा सकता है। ‘अध्ययन’ और ‘अध्यापन’ को निरंतर शिक्षा प्राप्त करने और ज्ञान साझा करने के रूप में देखा जा सकता है। ‘यजन’ और ‘याजन’ को व्यक्तिगत और सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्वों, नैतिक कार्यों तथा सामुदायिक सेवा के रूप में समझा जा सकता है। ‘दान’ और ‘प्रतिग्रह’ का महत्व परोपकार, सामाजिक न्याय और संसाधनों के उचित वितरण में आज भी उतना ही है। ये सिद्धांत व्यक्ति को एक संतुलित, नैतिक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में सहायता करते हैं।