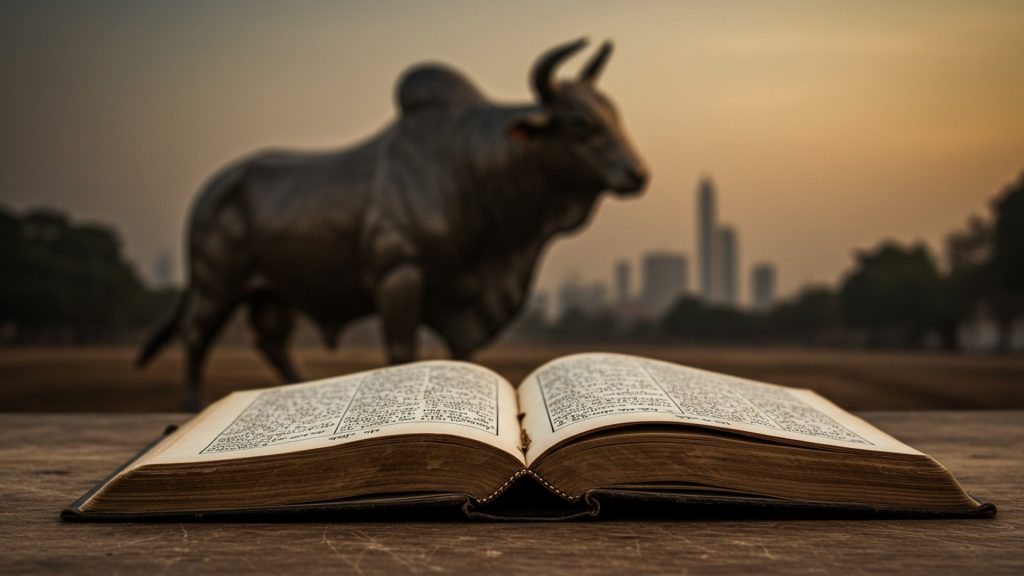हाल ही में मनुस्मृति के वृषभ विधानों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसने पशु कल्याण कार्यकर्ताओं और कुछ धार्मिक संगठनों को आमने-सामने ला दिया है। यह बहस प्राचीन ग्रंथों में बैलों से संबंधित वर्णित नियमों और आधुनिक पशु अधिकारों के मानकों के बीच बढ़ते टकराव पर केंद्रित है। देशभर में यह मुद्दा पशुओं के प्रति व्यवहार और सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं के बीच संतुलन साधने की आवश्यकता पर गंभीर सवाल उठा रहा है। मौजूदा घटनाक्रमों में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि क्या पशुओं के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता और अधिकारों की वकालत के दौर में ये ऐतिहासिक नियम आज के समाज में लागू किए जा सकते हैं।
हालिया विवाद का क्या है मामला?
हाल के दिनों में, प्राचीन हिंदू विधि ग्रंथ मनुस्मृति में वर्णित वृषभ (बैल) से संबंधित विधानों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह बहस इस सवाल पर केंद्रित है कि क्या सदियों पुराने ये नियम आज के पशु कल्याण कानूनों और आधुनिक नैतिकता के साथ मेल खाते हैं या उनमें टकराव है। यह मुद्दा विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। इस विवाद ने देश के प्राचीन मूल्यों और आधुनिक प्रगतिशील सोच के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को सामने ला दिया है।
मनुस्मृति में पशुओं के प्रति क्या है दृष्टिकोण?
मनुस्मृति, जिसे प्राचीन भारतीय कानून और सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, उसमें पशुओं के प्रति व्यवहार को लेकर अलग-अलग बातें कही गई हैं। एक ओर, कई श्लोक अहिंसा और जीवमात्र के प्रति दया का संदेश देते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि मनुस्मृति में हिंसा का निषेध किया गया है और जीवों को बांधने, मारने या क्लेश देने की इच्छा न रखने वाले को सुख पाने वाला बताया गया है। उदाहरण के लिए, एक श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी प्राणी को मारने की अनुमति देता है, मांस काटता है, पशु-पक्षी को मारता है, मारने के लिए मोल लेता या बेचता है, मांस पकाता है, परोसता है या खाता है, वे सभी हत्यारे और पापी होते हैं। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि मनुस्मृति में पशुओं की हिंसा को अनुचित माना गया है।
हालांकि, मनुस्मृति के कुछ अन्य श्लोकों में विशेष परिस्थितियों, जैसे यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं के उपयोग या मांस भक्षण का भी उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए, अध्याय 5 के एक श्लोक में कहा गया है कि “खाने लायक पशुओं का मांस खाना पाप नहीं है क्योंकि ब्रह्मा ने मांस खाने वाले और मांस खाने योग्य पशुओं दोनों को बनाया है।” कुछ व्याख्याकारों का मानना है कि ये श्लोक बाद में जोड़े गए (प्रक्षिप्त) हो सकते हैं, क्योंकि मनु का मूल सिद्धांत अहिंसा पर आधारित था और उन्होंने यज्ञ को ‘अध्वर’ यानी हिंसा रहित बताया था। वैदिक काल में भी गौवंश को मानव सभ्यता के लिए आवश्यक और पूज्य माना गया है।
वृषभ यानी बैलों के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय समाज में उनका उपयोग मुख्य रूप से कृषि और परिवहन जैसे कार्यों के लिए होता था। वैदिक सभ्यता में बैलों का बधियाकरण कर उन्हें खेतों और आवागमन में काम में लेने का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में सीधे तौर पर वृषभों के लिए विशेष “विधान” बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं हैं, लेकिन पशुओं के प्रति सामान्य दया या विशेष अनुष्ठानों में उनके उपयोग के नियम उन पर भी लागू होते हैं। यह दोहरी प्रकृति ही आज के विवाद का मूल है।
आधुनिक भारत के पशु कल्याण कानून
आधुनिक भारत ने पशुओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं, जो प्राचीन ग्रंथों की व्याख्याओं से अलग एक स्पष्ट कानूनी ढाँचा प्रदान करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960’ (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960), जिसे संसद द्वारा 1960 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या कष्ट से बचाना है।
इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- यह कानून पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता को अपराध मानता है और इसमें कई प्रकार की क्रूरता को परिभाषित किया गया है, जैसे पीटना, यातना देना, या अनावश्यक दर्द पहुँचाना।
- बीमार या घायल पशुओं से काम करवाना, उन्हें भोजन-पानी न देना, या पशुओं की लड़ाई को बढ़ावा देना भी इस अधिनियम के तहत अपराध है।
- इस अधिनियम की धारा 4 के तहत 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India – AWBI) का गठन किया गया, जो इन नियमों को लागू कराने और पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
- पहली बार अपराध करने पर 10 रुपये से 50 रुपये तक का जुर्माना लग सकता था, हालांकि हाल के संशोधनों में जुर्माने और कारावास को काफी बढ़ाने का प्रस्ताव है (75,000 रुपये तक का जुर्माना या 5 साल तक की जेल)।
- यह अधिनियम वैज्ञानिक प्रयोगों में इस्तेमाल होने वाले जानवरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है और निर्धारित करता है कि ऐसे प्रयोग केवल ज्ञान बढ़ाने या मानव और जानवरों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ही हो सकते हैं, और वे भी समिति की निगरानी में होने चाहिए।
भारतीय संविधान भी पशु कल्याण को महत्व देता है। अनुच्छेद 51(A) के अनुसार, हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के साथ-साथ देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन’ शब्द की व्याख्या को व्यापक करते हुए उसमें पशु जीवन को भी शामिल किया है, जिससे पशुओं को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलता है।
प्राचीन और आधुनिक नियमों के बीच टकराव
मनुस्मृति के वृषभ विधानों (और व्यापक रूप से पशुओं के प्रति नियमों) तथा आधुनिक पशु कल्याण कानूनों के बीच टकराव के कई बिंदु हैं:
-
पशुओं के उपयोग की सीमा:
मनुस्मृति में कुछ संदर्भ ऐसे हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों या विशेष अवसरों पर पशु बलि या मांस के सेवन की अनुमति देते प्रतीत होते हैं। इसके विपरीत, आधुनिक पशु कल्याण कानून पशुओं को अनावश्यक पीड़ा से बचाने पर केंद्रित हैं, और कुछ अनुष्ठानों में होने वाली क्रूरता को दंडनीय अपराध मानते हैं।
-
कानूनी प्रवर्तन बनाम धार्मिक व्याख्या:
आधुनिक कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और उनका उल्लंघन दंडनीय है। जबकि मनुस्मृति के नियम धार्मिक या नैतिक सिद्धांतों के रूप में देखे जाते हैं, जिनकी व्याख्या समय और परंपरा के अनुसार बदलती रही है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 28 धार्मिक प्रथाओं के तहत पशुओं को मारने को कुछ मामलों में अपराध नहीं मानती है, लेकिन यह धारा भी अक्सर बहस का विषय रहती है।
-
अधिकार बनाम कर्तव्य:
आधुनिक पशु कल्याण कानून पशुओं को ‘अधिकार’ प्रदान करते हैं, जैसे गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, पीड़ा से मुक्ति का अधिकार। वहीं, मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथ मुख्य रूप से मनुष्य के ‘कर्तव्यों’ पर जोर देते हैं, जिसमें पशुओं के प्रति दया भी शामिल है, लेकिन यह अधिकार के रूप में परिभाषित नहीं है जैसा कि आधुनिक कानून में है।
यह टकराव तब और गहरा हो जाता है जब कुछ प्राचीन प्रथाएं, जैसे कि वृषभों का अत्यधिक बोझ उठाने में उपयोग या उनके प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता, आधुनिक संवेदनशीलता और कानूनी मानदंडों के खिलाफ जाती हैं।
विभिन्न पक्षों के विचार
इस विवाद पर समाज के विभिन्न वर्गों की अलग-अलग राय है:
पशु अधिकार कार्यकर्ता: “हमारा मानना है कि पशुओं को अनावश्यक पीड़ा से बचाना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या आधुनिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए, और किसी भी परंपरा के नाम पर पशु क्रूरता को जायज नहीं ठहराया जा सकता।”
धार्मिक विद्वान: “मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ है जिसकी कई व्याख्याएं हैं। इसमें अहिंसा के भी महत्वपूर्ण उपदेश हैं। हमें यह समझना होगा कि समय के साथ सामाजिक मानदंड बदलते हैं। मूल भावना पशुओं के प्रति करुणा की है, न कि क्रूरता की। कुछ श्लोक बाद के काल में जोड़े गए हो सकते हैं।”
कानूनी विशेषज्ञ: “भारत का संविधान और ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम’ देश के सर्वोच्च कानून हैं। किसी भी प्राचीन पाठ या परंपरा की व्याख्या इन कानूनों के दायरे में होनी चाहिए। न्यायपालिका ने भी बार-बार पशु अधिकारों को वरीयता दी है, भले ही वह लोकप्रिय मान्यताओं या परंपराओं के खिलाफ हो।”
कुछ लोग तर्क देते हैं कि प्राचीन ग्रंथों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए और उन्हें सीधे आधुनिक कानूनों से जोड़ना उचित नहीं है। वहीं, कुछ अन्य लोग मानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों की ऐसी व्याख्याओं को खारिज कर देना चाहिए जो आधुनिक समाज के मानवीय और नैतिक मूल्यों के खिलाफ हैं।
आगे की राह और संभावनाएं
मनुस्मृति के वृषभ विधानों और आधुनिक पशु कल्याण कानूनों के बीच का यह विवाद एक जटिल मुद्दा है, जिसके लिए सोच-समझकर समाधान की आवश्यकता है। आगे की राह में कई पहलू शामिल हो सकते हैं:
-
जन जागरूकता:
पशु कल्याण कानूनों और उनके महत्व के बारे में आम लोगों में अधिक जागरूकता फैलाना आवश्यक है। इससे पशुओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा।
-
कानूनी सुधार:
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में प्रस्तावित संशोधन, जिनमें जुर्माने और सजा को बढ़ाया गया है, पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने में मदद कर सकते हैं।
-
धार्मिक संवाद:
धार्मिक नेताओं और विद्वानों के बीच संवाद स्थापित करना महत्वपूर्ण है, ताकि प्राचीन ग्रंथों की ऐसी व्याख्याएं प्रस्तुत की जा सकें जो अहिंसा और करुणा के मूल सिद्धांतों पर आधारित हों और आधुनिक पशु कल्याण के साथ संगत हों।
-
न्यायपालिका की भूमिका:
न्यायपालिका ने पहले भी कई बार पशु अधिकारों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भविष्य में भी, ऐसे मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण होगा।
यह आवश्यक है कि समाज अपने समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का सम्मान करे, लेकिन साथ ही साथ आधुनिक नैतिक और कानूनी मानदंडों के प्रति भी प्रतिबद्ध रहे। पशु कल्याण केवल कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जो सभी जीवित प्राणियों के साथ दयालु व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। इस विवाद का समाधान एक संतुलित दृष्टिकोण से ही संभव है, जहाँ प्राचीन ज्ञान और आधुनिक प्रगतिशील सोच का संगम हो सके।