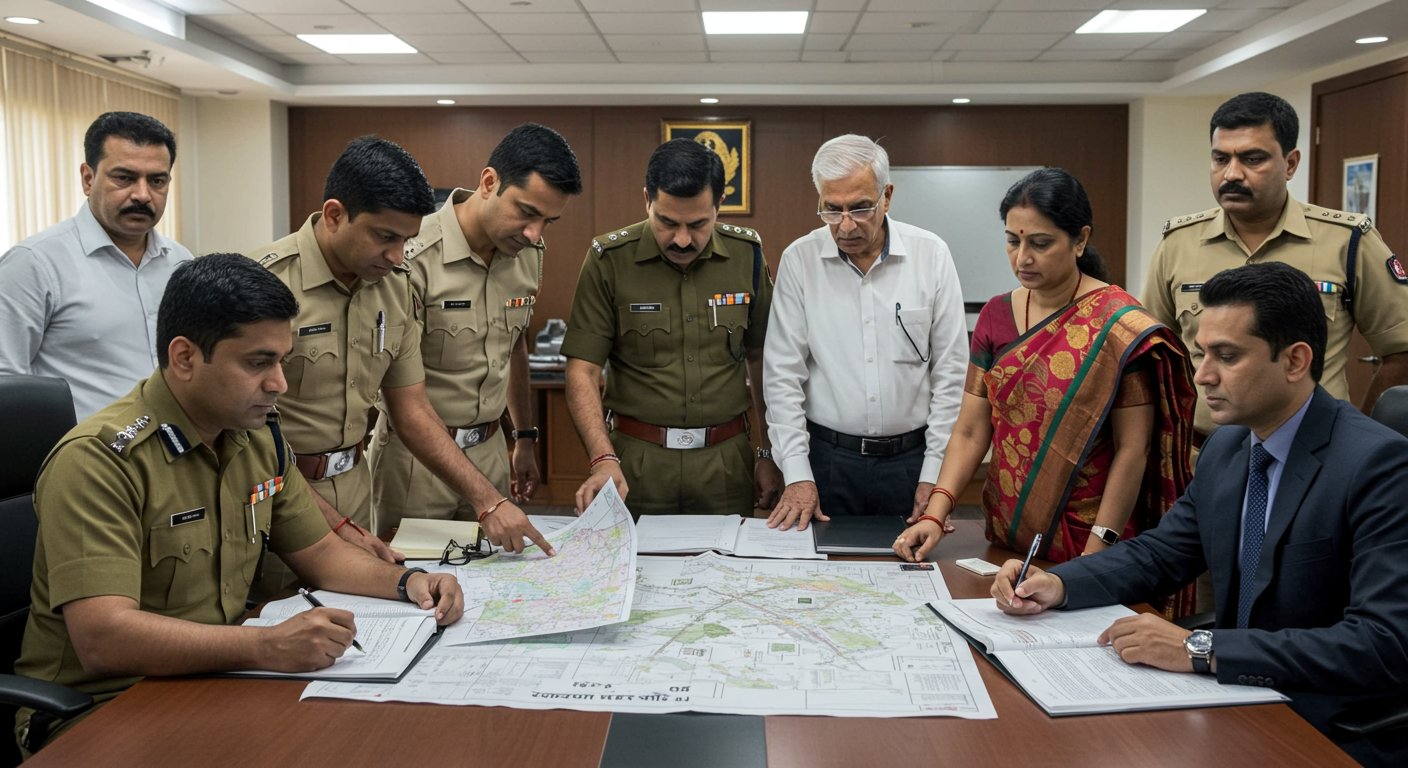आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रम पर बात करेंगे जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन की मृत्यु की और उसके बाद भारत में हुई सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। वही माउंटबेटन, जिन्होंने भारत-पाकिस्तान के बंटवारे में एक अहम भूमिका निभाई थी और जिसके कारण लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा था। तो फिर क्यों उनकी मौत पर, बंटवारे का दर्द झेल चुके भारत में, इतने बड़े स्तर पर शोक मनाया गया?
यह बात 1979 की है, जब आयरलैंड में हुए एक आतंकी हमले में लॉर्ड माउंटबेटन की दुखद मृत्यु हो गई। इस खबर से ब्रिटेन में तो गहरा दुख था ही, लेकिन दुनिया को तब सबसे ज्यादा हैरानी हुई जब भारत सरकार ने भी उनके सम्मान में सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी। देश के झंडे आधे झुका दिए गए और कई सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। अखबारों में यह खबर छाई रही और आम लोगों के मन में यह सवाल उठता रहा कि आखिर जिस शख्स को भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार माना जाता था, उसकी मौत पर देश ने इतना सम्मान क्यों दिखाया? इसके पीछे क्या कारण थे, यह जानना दिलचस्प है।
लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, जिन्हें देश को आजादी दिलाने और सत्ता का हस्तांतरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन, उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा और विवादास्पद फैसला भारत का बंटवारा था, जिसने उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। माउंटबेटन ने बहुत जल्दबाजी में विभाजन की योजना को अंजाम दिया। उन्होंने रेडक्लिफ रेखा खींचने के लिए सिर्फ कुछ हफ्तों का समय दिया, जिसके कारण लाखों लोग अपने घर-बार छोड़ने पर मजबूर हुए और बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की। इस विभाजन में अनुमानित 10 लाख लोग मारे गए और करोड़ों विस्थापित हुए।
उनकी विरासत पर हमेशा बहस होती रही है। एक तरफ, उन्हें भारत की आजादी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ, उन्हें भारत-पाकिस्तान बंटवारे और उसके भयानक नतीजों का मुख्य जिम्मेदार भी माना जाता है। आलोचकों का कहना है कि उन्होंने ब्रिटेन के हितों को पहले रखा और एक जटिल समस्या का जल्दबाजी में, अधूरा समाधान दिया। फिर भी, उनकी मृत्यु पर भारत में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया, जो सत्ता हस्तांतरण में उनकी भूमिका और एक स्वतंत्र राष्ट्र के प्रति उनकी औपचारिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, भले ही उनके फैसले कितने भी विवादास्पद रहे हों।
भारत का विभाजन करने वाले लॉर्ड माउंटबेटन की मौत एक चौंकाने वाली घटना थी, जिसने दुनियाभर में सुर्खियाँ बटोरीं। 27 अगस्त 1979 को आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (IRA) ने उनकी नाव में बम लगाकर उन्हें मार डाला था। इस हमले में माउंटबेटन के साथ उनके परिवार के कुछ और लोग भी मारे गए।
यह घटना तब और खास हो गई जब भारत ने उनकी मौत पर सात दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। कई लोगों के लिए यह बात समझ से परे थी कि जिस व्यक्ति ने भारत के दो टुकड़े किए, जिससे लाखों लोगों को विस्थापन और हिंसा झेलनी पड़ी, उसकी मौत पर भारत इतना सम्मान क्यों दिखा रहा है। हालांकि, भारत सरकार का मानना था कि भले ही विभाजन का दर्द कड़वा था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत को सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से किया था। वे भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर-जनरल थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कई भारतीय नेताओं के साथ उनके निजी संबंध काफी अच्छे थे। इसलिए, भारत ने उन्हें सम्मानजनक विदाई दी, जो एक अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है।
जनमानस में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन का मुख्य जिम्मेदार माना जाता है, जिसने लाखों लोगों के जीवन में उथल-पुथल मचा दी थी। ऐसे में, जब उनकी मृत्यु पर भारत में सात दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि जिसने देश को बांटा, उसके लिए इतना सम्मान क्यों? जनमानस की यह धारणा आज भी कायम है कि विभाजन का दर्द गहरा था और ऐसे में शोक मनाना विरोधाभासी लगता है।
ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि यह फैसला जटिल परिस्थितियों में लिया गया था। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल थे और उनका भारतीय नेताओं, खासकर जवाहरलाल नेहरू के साथ एक खास रिश्ता था। आधिकारिक स्तर पर, उनकी भूमिका को ‘सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण’ में महत्वपूर्ण माना गया। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह सरकारी स्तर पर लिया गया एक कूटनीतिक और राजनीतिक फैसला था, न कि पूरे देश की आम भावना का प्रतिबिंब। उस समय सरकार अंतरराष्ट्रीय संबंधों और प्रोटोकॉल का पालन कर रही थी, जबकि आम जनता अभी भी विभाजन के भयानक परिणामों से जूझ रही थी। यह दर्शाता है कि सरकारी निर्णय और जनमानस की भावनाओं के बीच एक स्पष्ट अंतर था।
माउंटबेटन की मृत्यु पर भारत में सात दिन का राजकीय शोक घोषित करना, उस समय की जटिल राजनीति और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था। कई लोगों के लिए यह विरोधाभासी लग सकता है कि जिस व्यक्ति ने भारत का विभाजन किया, उसके लिए शोक क्यों मनाया गया। हालांकि, यह कदम भविष्य की पीढ़ियों के लिए कई कूटनीतिक निहितार्थ और महत्वपूर्ण सबक छोड़ गया। भारत के तत्कालीन नेतृत्व, खासकर पंडित नेहरू ने, माउंटबेटन के साथ अपने व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को एक व्यापक कूटनीतिक दायरे में देखा। यह ब्रिटेन के साथ नए-नए स्वतंत्र हुए भारत के संबंधों को मजबूत करने का एक तरीका था, खासकर जब भारत एक नई अंतरराष्ट्रीय पहचान बना रहा था।
एक नए राष्ट्र के रूप में भारत दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि वह इतिहास की कड़वाहट से ऊपर उठकर अंतरराष्ट्रीय संबंध बना सकता है। यह निर्णय केवल तात्कालिक कूटनीति से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह भारत की विदेश नीति की नींव भी बना। इसने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अपने गौरवशाली अतीत को याद रखते हुए भी भविष्योन्मुखी सोच रखता है। भावी पीढ़ियों को यह समझना चाहिए कि राष्ट्रहित और वैश्विक संबंधों को बनाए रखने के लिए कभी-कभी व्यक्तिगत भावनाओं या ऐतिहासिक असहमतियों से ऊपर उठना पड़ता है। यह परिपक्व राजनीति और दूरदर्शिता का उदाहरण था, जिसने एक युवा राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया और यह दिखाया कि जटिल ऐतिहासिक घटनाओं के बावजूद, कूटनीति और समझदारी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है।
तो आखिर क्यों मनाया गया माउंटबेटन की मौत पर शोक? यह फैसला सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों का नहीं, बल्कि नव स्वतंत्र भारत की गहरी कूटनीतिक सूझबूझ का प्रतीक था। इसने दिखाया कि भारत इतिहास की कड़वाहट से ऊपर उठकर भी वैश्विक संबंध बनाने और एक परिपक्व राष्ट्र के रूप में पहचान स्थापित करने में सक्षम था। यह हमें सिखाता है कि राष्ट्रहित और अंतरराष्ट्रीय सम्मान के लिए कभी-कभी ऐतिहासिक असहमतियों से ऊपर उठना पड़ता है। यह युवा राष्ट्र की दूरदर्शिता का एक महत्वपूर्ण सबक था।