मनुष्य जीवन में अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझना सदियों से एक गूढ़ प्रश्न रहा है। क्या हमारे वर्तमान सुख-दुःख पिछली गतिविधियों का प्रतिफल हैं, और क्या हमारे आज के कार्य हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं? भारतीय दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत इस जटिल पहेली को सुलझाता है, और इन अवधारणाओं को गहराई से समझने के लिए मनुस्मृति एक अद्वितीय स्रोत प्रस्तुत करती है। यह प्राचीन धर्मशास्त्र न केवल कर्म के सूक्ष्म नियमों को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे प्रत्येक क्रिया, चाहे शुभ हो या अशुभ, आत्मा की यात्रा को अगले जन्मों तक प्रभावित करती है। मनुस्मृति के अनुसार, जीवन का चक्र सिर्फ एक भौतिक अस्तित्व नहीं, बल्कि कर्मों की एक अटूट श्रृंखला है जो हमारे आध्यात्मिक गंतव्य को आकार देती है।
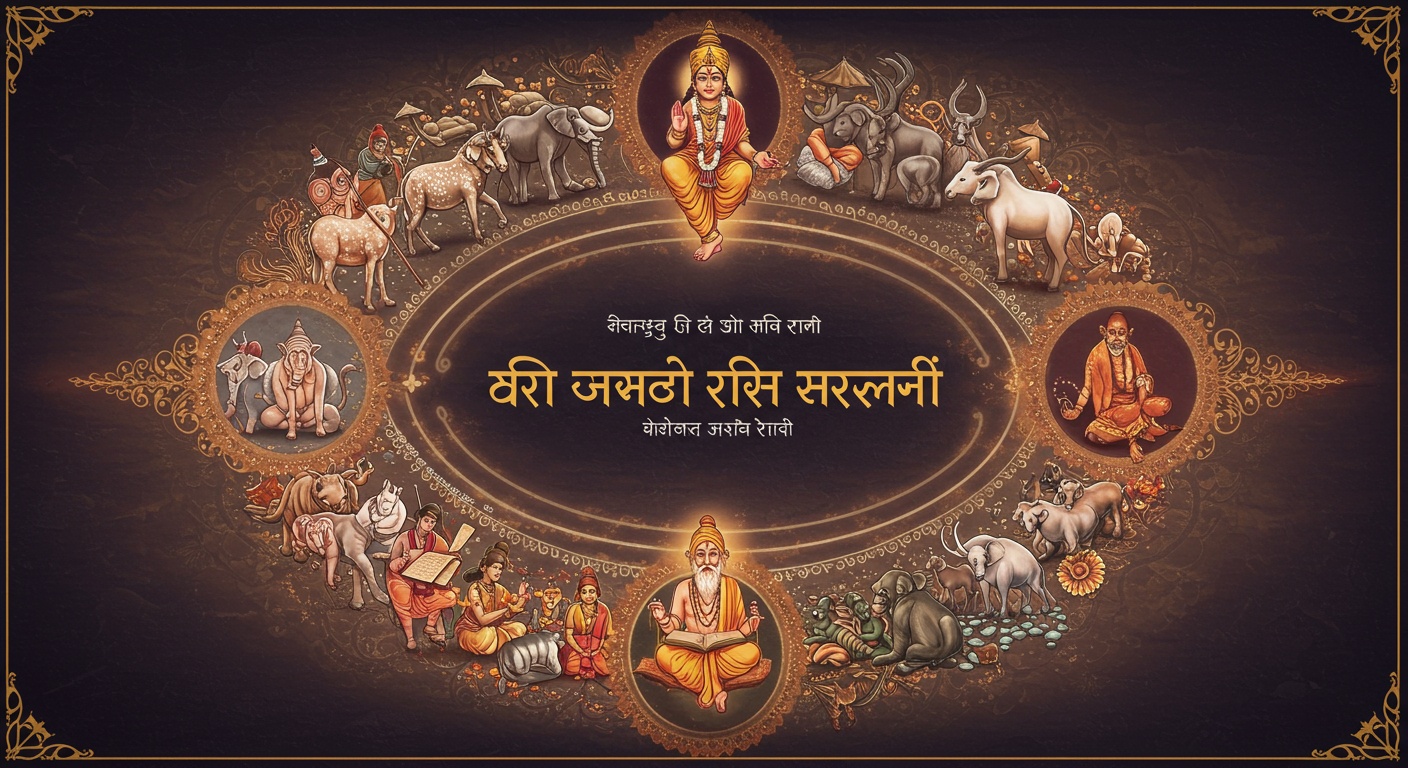
कर्म का मौलिक सिद्धांत और उसका पुनर्जन्म से जुड़ाव
भारतीय दर्शन में ‘कर्म’ केवल किसी क्रिया का नाम नहीं, बल्कि यह एक गहन सिद्धांत है जो हमारे हर विचार, शब्द और कार्य के परिणामों को समाहित करता है। यह एक लौकिक नियम है जो कहता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, उसका हमारे वर्तमान और भविष्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है।
कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म की अवधारणा से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई कर्म करते हैं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, उसका एक ‘संस्कार’ या ‘वासना’ (छाप या प्रवृत्ति) हमारी आत्मा पर अंकित हो जाती है। ये संस्कार ही हमारी भविष्य की इच्छाओं, व्यक्तित्व और अनुभवों का निर्माण करते हैं। यदि इस जीवन में हमारे सभी कर्मों के फल पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं, या हमारी इच्छाएँ अधूरी रह जाती हैं, तो आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है ताकि उन कर्मों के फलों का अनुभव कर सके और उन इच्छाओं को पूरा कर सके। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती, अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो जाती।
सरल शब्दों में, कर्म वह बीज है जो हम बोते हैं, और पुनर्जन्म वह खेत है जहाँ हम उन बीजों के फल काटते हैं। यह निरंतरता सुनिश्चित करती है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता और हर जीव अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदार है। यह जीवन को नैतिक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने की प्रेरणा देता है।
पुनर्जन्म की अवधारणा: क्यों और कैसे?
पुनर्जन्म, जिसे आवागमन या आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन भी कहा जाता है, भारतीय दर्शन की एक मूलभूत अवधारणा है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है, आत्मा अमर है और यह अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है।
- क्यों होता है पुनर्जन्म?
- अधूरे कर्मफल: इस जीवन में किए गए सभी कर्मों के फल इसी जन्म में अनुभव नहीं किए जा सकते। शेष कर्मों के फल भोगने के लिए आत्मा को नया शरीर धारण करना पड़ता है।
- अधूरी इच्छाएँ और वासनाएँ: मनुष्य की अनेक इच्छाएँ और वासनाएँ इस जीवन में पूरी नहीं हो पातीं। इन वासनाओं के कारण आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है ताकि वे पूरी हो सकें।
- मोक्ष की प्राप्ति तक: जब तक आत्मा को आत्मज्ञान नहीं होता और वह कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाती, तब तक वह जन्म-मृत्यु के चक्र में फँसी रहती है।
- कैसे होता है पुनर्जन्म?
जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो सूक्ष्म शरीर (जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार होते हैं) आत्मा के साथ यात्रा करता है। यह सूक्ष्म शरीर ही पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा-जोखा अपने साथ ले जाता है। इन संचित कर्मों और इच्छाओं के आधार पर ही आत्मा को अगली योनि (प्रजाति या जीवन का रूप) प्राप्त होती है। यह निर्धारण न केवल मानव योनि तक सीमित है, बल्कि पशु, पक्षी या अन्य योनियों में भी हो सकता है, जो व्यक्ति के कर्मों की प्रकृति पर निर्भर करता है।
यह प्रक्रिया एक जटिल प्रणाली है जहाँ सूक्ष्म कर्मफल (अदृष्ट) अगली योनि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ लोग जन्म से ही विशिष्ट परिस्थितियों या क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं, जबकि अन्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सब उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल माना जाता है।
मनुस्मृति में कर्म और पुनर्जन्म का विस्तृत विवेचन
भारतीय विधि और नैतिकता के प्राचीन ग्रंथ, मनुस्मृति, में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को अत्यंत विस्तार से समझाया गया है। यह ग्रंथ न केवल सामाजिक व्यवस्थाओं को परिभाषित करता है, बल्कि व्यक्ति के नैतिक आचरण और उसके आगामी जन्मों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी गहन प्रकाश डालता है। मनुस्मृति के अनुसार, कर्मों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है: शारीरिक, वाचिक और मानसिक।
- शारीरिक कर्म (काया से किए गए): ये वे कर्म हैं जो शरीर द्वारा किए जाते हैं, जैसे हिंसा, चोरी, व्यभिचार। मनुस्मृति स्पष्ट करती है कि ऐसे कर्मों के नकारात्मक परिणाम व्यक्ति को निम्न योनियों में ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मनुस्मृति (12. 9) में कहा गया है कि चोर, हिंसक और व्यभिचारी जैसे लोग निम्न योनियों में जन्म लेते हैं।
- वाचिक कर्म (वाणी से किए गए): इसमें झूठ बोलना, कटु वचन कहना, चुगली करना या किसी की निंदा करना शामिल है। मनुस्मृति बताती है कि वाणी के दुरुपयोग से भी आत्मा को अगले जन्म में कष्ट भोगने पड़ते हैं। वाणी की शुद्धता पर बहुत जोर दिया गया है।
- मानसिक कर्म (मन से किए गए): ये सबसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण कर्म होते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, लोभ या दूसरों के धन की लालसा जैसे मानसिक पाप व्यक्ति के भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं। मनुस्मृति (12. 3) के अनुसार, मानसिक शुद्धता ही सर्वोच्च धर्म है, क्योंकि मन की शुद्धि से ही वाणी और शरीर शुद्ध होते हैं।
मनुस्मृति पाप (अशुभ कर्म) और पुण्य (शुभ कर्म) के संचय के आधार पर आत्मा के विभिन्न योनियों में गमन का विस्तृत वर्णन करती है। यह ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताता है कि धर्म (नैतिकता और कर्तव्य) का पालन करने वाले व्यक्ति उच्च योनियों (जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) में जन्म लेते हैं, जबकि अधर्म का आचरण करने वाले निम्न योनियों (जैसे पशु, पक्षी, कीट) में जन्म लेते हैं। यह अवधारणा व्यक्ति को धर्मानुकूल जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, यह जानते हुए कि उनके वर्तमान कर्मों का सीधा संबंध उनके भविष्य के अस्तित्व से है। मनुस्मृति इस बात पर भी जोर देती है कि ज्ञान और तपस्या के माध्यम से व्यक्ति इन कर्मबंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ सकता है।
विभिन्न प्रकार के कर्म और उनके फल (मनुस्मृति के अनुसार)
मनुस्मृति में कर्मों को उनकी प्रकृति और परिणामों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो पुनर्जन्म के चक्र को समझने में मदद करता है। यह वर्गीकरण व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति अधिक सचेत रहने की प्रेरणा देता है।
| कर्म का प्रकार | विवरण | मनुस्मृति के अनुसार संभावित फल / पुनर्जन्म पर प्रभाव |
|---|---|---|
| सकाम कर्म | फल की इच्छा से किए गए कर्म (जैसे स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ, धन के लिए व्यापार)। | इन कर्मों के फल स्वरूप व्यक्ति को स्वर्ग या अन्य सुखमय लोक प्राप्त हो सकते हैं, परंतु जब तक फल समाप्त नहीं होता, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। यह चक्र को जारी रखता है। |
| निष्काम कर्म | बिना किसी फल की इच्छा के, केवल कर्तव्य मानकर किए गए कर्म (जैसे निःस्वार्थ सेवा, धर्म का पालन)। | ये कर्म आत्मा को बंधन से मुक्त करने में सहायक होते हैं। ये मोक्ष की ओर ले जाते हैं और पुनर्जन्म के चक्र को कमजोर करते हैं। |
| नित्य कर्म | प्रतिदिन किए जाने वाले अनिवार्य कर्म (जैसे संध्या वंदन, अग्निहोत्र)। | इनका पालन न करने पर पाप लगता है, जबकि पालन करने पर कोई विशेष फल नहीं मिलता, बल्कि यह धर्म का आधार बनता है और व्यक्ति को नैतिक रूप से शुद्ध रखता है। |
| नैमित्तिक कर्म | विशेष अवसरों पर किए जाने वाले कर्म (जैसे संस्कारों के लिए यज्ञ, श्राद्ध)। | ये कर्म विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होते हैं और इनके अनुष्ठान से पुण्य की प्राप्ति होती है, जो अगले जन्म की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। |
| पाप कर्म | धर्म विरुद्ध, अनैतिक और निंदनीय कर्म (जैसे चोरी, हत्या, झूठ)। | मनुस्मृति के अनुसार, ऐसे कर्म व्यक्ति को निम्न योनियों (पशु, पक्षी, कीट आदि) में जन्म लेने पर विवश करते हैं और उसे घोर कष्ट भोगने पड़ते हैं। |
| प्रायश्चित कर्म | किए गए पापों के शोधन के लिए किए जाने वाले कर्म या अनुष्ठान। | ये कर्म पापों के प्रभाव को कम करने या नष्ट करने में मदद करते हैं, जिससे अगले जन्म की कष्टप्रद स्थितियाँ कम हो सकती हैं। यह आत्म-शुद्धि का मार्ग है। |
यह वर्गीकरण दर्शाता है कि मनुस्मृति कर्मों के सूक्ष्म भेदों और उनके दूरगामी परिणामों पर कितना जोर देती है। यह हमें सिखाता है कि हमारे हर छोटे-बड़े कर्म का महत्व है और वे हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं।
कर्मफल का संचय और अगली योनि का निर्धारण
कर्मफल का संचय एक ऐसी अदृश्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे सभी कर्मों के सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर अंकित होते चले जाते हैं। इसे ‘अदृष्ट’ या ‘संस्कार’ कहा जाता है। ये संस्कार सिर्फ इस जन्म के नहीं, बल्कि अनगिनत पिछले जन्मों के कर्मों का कुल योग होते हैं। जब एक जीवन का अंत होता है, तो भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अपने साथ इन संचित कर्मफलों (वासनाओं और संस्कारों) को लेकर आगे बढ़ती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक कंप्यूटर अपनी हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को सहेज कर रखता है, भले ही उसकी स्क्रीन बंद हो जाए।
मनुस्मृति के अनुसार, इन संचित कर्मफलों के आधार पर ही आत्मा की अगली योनि (नया जन्म) निर्धारित होती है। यह निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है:
- कर्मों की प्रकृति: शुभ, अशुभ या मिश्रित कर्मों के आधार पर।
- सत्त्व गुण प्रधान कर्म: ज्ञान, दान, अहिंसा जैसे कर्म व्यक्ति को उच्च मानव योनियों, विद्वानों के घरों या देवताओं के लोकों में जन्म दिलाते हैं।
- रजोगुण प्रधान कर्म: तीव्र इच्छा, महत्वाकांक्षा, संघर्ष जैसे कर्म व्यक्ति को मध्यम मानव योनियों में, व्यापारियों या योद्धाओं के रूप में जन्म दिलाते हैं।
- तमोगुण प्रधान कर्म: अज्ञान, आलस्य, हिंसा, अनैतिकता जैसे कर्म व्यक्ति को निम्न योनियों (पशु, पक्षी, कीट) या निम्न मानव वर्ग में जन्म दिलाते हैं।
- इच्छाएँ और वासनाएँ: मृत्यु के समय प्रबल इच्छाएँ और वासनाएँ भी अगले जन्म की दिशा निर्धारित करती हैं। यदि व्यक्ति की इच्छाएँ भौतिक सुखों से बंधी थीं, तो उसे फिर से ऐसे शरीर में जन्म लेना पड़ सकता है जहाँ वह उन इच्छाओं को पूरा कर सके।
- अदृष्ट का प्रभाव: ‘अदृष्ट’ वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप बनती है और हमें उन परिणामों को भोगने के लिए एक विशेष शरीर और परिस्थितियाँ प्रदान करती है। यह अदृश्य शक्ति ही यह तय करती है कि व्यक्ति किस परिवार में, किस देश में, किस लिंग में और किस तरह के शारीरिक व मानसिक गुणों के साथ जन्म लेगा।
उदाहरण के लिए, मनुस्मृति (12. 42-45) में विशिष्ट पापों के लिए विशिष्ट योनियों का उल्लेख मिलता है। जैसे, गुरु की हत्या करने वाला चांडाल योनि में, स्वर्ण की चोरी करने वाला कीड़े-मकोड़े की योनि में, और मांस खाने वाला पशु योनि में जन्म ले सकता है। यह दर्शाता है कि मनुस्मृति कर्म और उसके फल के बीच सीधा और तार्किक संबंध स्थापित करती है, जिससे व्यक्ति को अपने वर्तमान कर्मों के प्रति अत्यधिक जिम्मेदार होने की प्रेरणा मिलती है।
मोक्ष का मार्ग और कर्म के बंधन से मुक्ति
कर्म और पुनर्जन्म के चक्र की समझ का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के इस निरंतर चक्र से पूर्ण मुक्ति, आत्मा का परम शांति और परमानंद की स्थिति में स्थित हो जाना। यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा कर्म के किसी भी बंधन से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाती है और उसे फिर से शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
मनुस्मृति सीधे तौर पर मोक्ष के विस्तृत मार्गों का वर्णन नहीं करती जैसे कि उपनिषद या योग दर्शन करते हैं, लेकिन यह धर्म, नैतिक आचरण और कर्तव्य पालन पर अत्यधिक जोर देती है, जो परोक्ष रूप से मोक्ष की दिशा में कदम माने जाते हैं। मनुस्मृति के अनुसार, धर्म का पालन करना, सदाचार का जीवन जीना, अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का निर्वहन करना, और मानसिक तथा शारीरिक शुद्धता बनाए रखना, ये सभी व्यक्ति को पापों से बचाते हैं और पुण्य का संचय करते हैं।
मोक्ष की ओर ले जाने वाले प्रमुख सिद्धांत और क्रियाएँ, जिनका मनुस्मृति में भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिलता है:
- निष्काम कर्म: फल की इच्छा के बिना केवल कर्तव्य मानकर कर्म करना। जब व्यक्ति कर्मों के फलों में आसक्ति छोड़ देता है, तो वह नए कर्म बंधन नहीं बनाता।
- आत्मज्ञान: अपनी वास्तविक प्रकृति को जानना, यह समझना कि आत्मा शरीर से भिन्न और अमर है। यह ज्ञान अज्ञानता को दूर करता है, जो कर्म और पुनर्जन्म का मूल कारण है।
- तपस्या और संयम: इंद्रियों पर नियंत्रण, त्याग और अनुशासन का पालन करना। यह मन को शुद्ध करता है और वासनाओं को कम करता है।
- धर्म का पालन: नैतिक और धार्मिक नियमों का कड़ाई से पालन करना। मनुस्मृति के अनुसार, धर्म ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है।
- प्रायश्चित: अनजाने या जानबूझकर किए गए पापों का प्रायश्चित करना। यह आत्मा पर पड़े नकारात्मक कर्मफलों के प्रभावों को कम करता है।
सार यह है कि यद्यपि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें अपने कार्यों के परिणामों के प्रति जिम्मेदार बनाता है, वहीं यह हमें यह आशा भी देता है कि हम अपने वर्तमान कर्मों को सुधार कर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। मनुस्मृति का संदेश स्पष्ट है: वर्तमान जीवन में किए गए धर्मानुकूल कार्य ही हमें जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करना, दूसरों के प्रति दयालु होना, और ईमानदारी से जीवन जीना ही इस कर्म-चक्र को तोड़ने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण ‘कार्य’ है।
निष्कर्ष
मनुस्मृति हमें स्पष्ट रूप से समझाती है कि हमारे कर्म ही हमारे पुनर्जन्म का आधार तय करते हैं। यह केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक व्यावहारिक दर्शन है। आज के युग में भी, जब हम सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी करते हैं या कोई व्यावसायिक निर्णय लेते हैं, तो उसके पीछे की हमारी नीयत और कार्यप्रणाली ही हमारे भविष्य के स्वरूप को गढ़ती है। मैंने स्वयं यह महसूस किया है कि जब हम छोटे से छोटे कार्य में भी ईमानदारी और नैतिकता रखते हैं, तो मन में एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास आता है। यह जागरूकता कि हर क्रिया का प्रतिफल है, हमें अधिक सचेत और जिम्मेदार बनाती है। तो आइए, आज से ही अपने हर कर्म को एक निवेश मानें – एक ऐसा निवेश जो न केवल इस जीवन को, बल्कि आने वाले जन्मों को भी उज्ज्वल बनाएगा। यही मनुस्मृति का सार है: अपने भविष्य के निर्माता स्वयं बनें।
अधिक लेख
सदाचार का महत्व: मनुस्मृति से सीखें उत्तम जीवन जीने के सूत्र
दैनिक जीवन में पवित्रता कैसे बनाए रखें मनुस्मृति से सीखें
पाप से मुक्ति के 4 आध्यात्मिक उपाय मनुस्मृति से सीखें
आत्मिक शुद्धिकरण का प्राचीन ज्ञान मनुस्मृति से सीखें
मनुस्मृति के अनुसार पापों से शुद्ध होने के 5 आवश्यक नियम
FAQs
मनुस्मृति के अनुसार कर्म और पुनर्जन्म का मूलभूत संबंध क्या है?
मनुस्मृति कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को बहुत गहराई से समझाती है। इसके अनुसार, व्यक्ति द्वारा इस जीवन में किए गए सभी कर्म (शुभ या अशुभ) उसके भविष्य के जन्म का निर्धारण करते हैं। यह एक अटूट संबंध है जहाँ कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनता है।
मनुस्मृति में कर्म की अवधारणा को कितनी महत्ता दी गई है?
मनुस्मृति में कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य का प्रत्येक कार्य उसके भाग्य का निर्माता होता है। कर्म ही व्यक्ति के अगले जन्म की योनि (जाति, प्रजाति) और उसके सुख-दुख का निर्णय करते हैं।
मनुस्मृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के कर्मों का क्या प्रभाव होता है?
मनुस्मृति शुभ (पुण्य), अशुभ (पाप) और मिश्रित कर्मों का उल्लेख करती है। शुभ कर्मों से व्यक्ति उच्च योनियों में जन्म लेता है और सुख भोगता है, जबकि अशुभ कर्मों से उसे निम्न योनियों (जैसे पशु, कीट) में जन्म मिलता है और दुख सहना पड़ता है। मिश्रित कर्मों से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, जहाँ सुख-दुख दोनों होते हैं।
पुनर्जन्म की प्रक्रिया को मनुस्मृति में किस प्रकार समझाया गया है?
मनुस्मृति बताती है कि आत्मा अमर है और वह शरीर त्यागने के बाद अपने संचित कर्मों के अनुसार एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन ही पुनर्जन्म है, और यह तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती।
मनुस्मृति अच्छे कर्मों पर इतना जोर क्यों देती है?
मनुस्मृति अच्छे कर्मों पर इसलिए जोर देती है क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है जिससे व्यक्ति न केवल इस जीवन में सुख और सम्मान प्राप्त कर सकता है, बल्कि भविष्य के जन्मों में भी बेहतर स्थिति प्राप्त कर सकता है। अच्छे कर्म ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है।
क्या मनुस्मृति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का कोई मार्ग सुझाती है?
हाँ, मनुस्मृति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति (मोक्ष) का मार्ग सुझाती है। यह धर्मानुसार जीवन जीने, स्वधर्म का पालन करने, तपस्या, ज्ञान प्राप्त करने और निस्वार्थ भाव से कर्म करने पर जोर देती है। इन मार्गों का अनुसरण करके व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
कर्मफल के निर्धारण में मनुस्मृति के अनुसार क्या व्यक्ति की नियत (इरादे) का भी कोई महत्व होता है?
हाँ, मनुस्मृति के अनुसार कर्म के फल में व्यक्ति की नियत (इरादे) का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि क्रिया के पीछे का विचार और भावना भी कर्मफल को निर्धारित करती है। शुद्ध नियत से किया गया कार्य शुभ फल देता है, जबकि दुर्भावना से किया गया कार्य अशुभ फल देता है, भले ही वह ऊपरी तौर पर अच्छा लगे।











