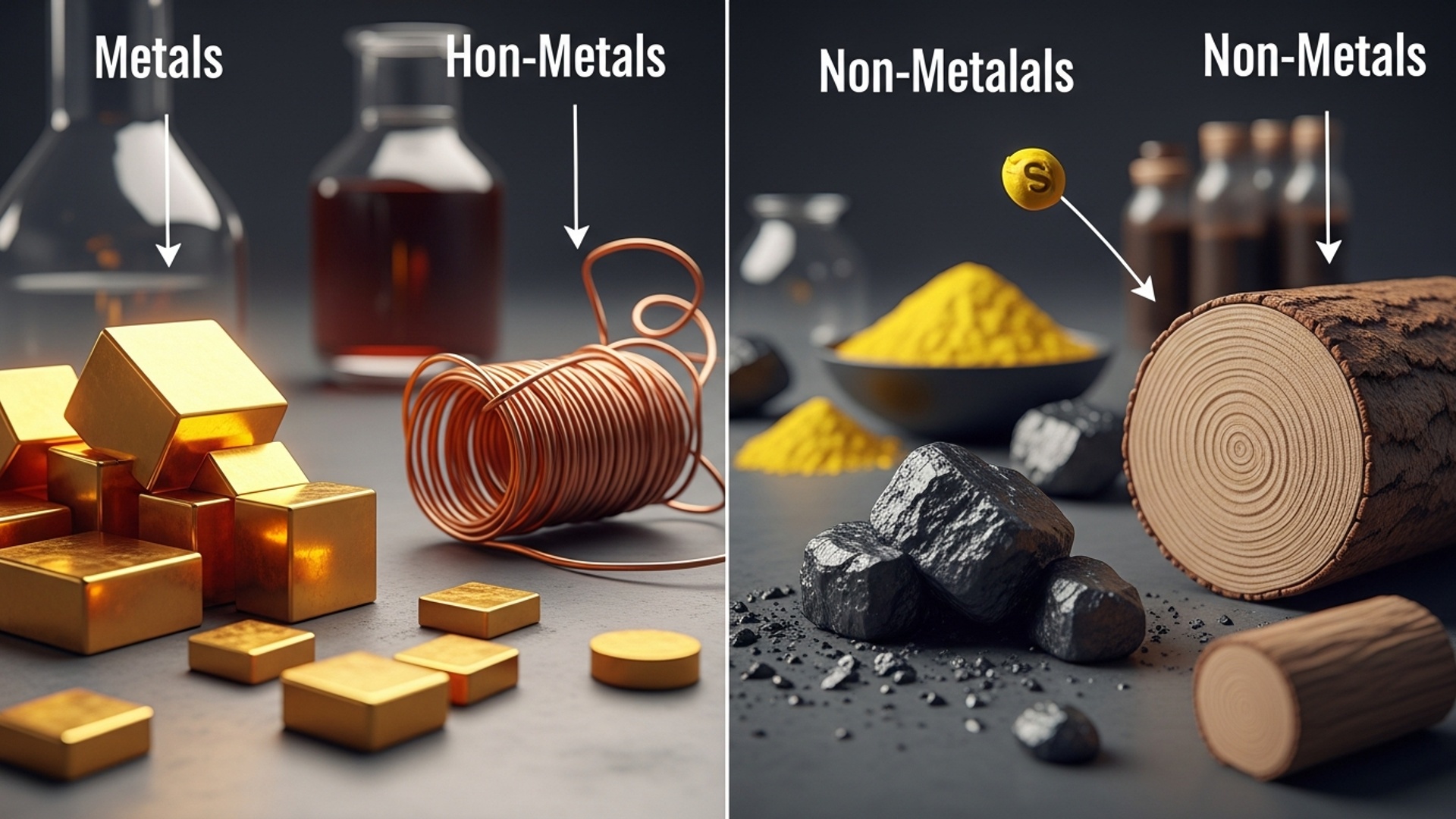आज के बदलते सामाजिक परिवेश में ‘धर्म’ की अवधारणा अक्सर भ्रमित करती है, जहाँ आधुनिक व्याख्याएँ और प्राचीन ग्रंथों की शाब्दिक समझ के बीच टकराव दिखता है। मनुस्मृति, जिसे सदियों से भारतीय जीवन-दर्शन का आधार माना गया है, कई बार विवादों का केंद्र रही है, खासकर जब इसके श्लोकों को उनके मूल संदर्भ से हटाकर देखा जाता है। उदाहरण के लिए, आज की नारीवादी बहसें या सामाजिक न्याय आंदोलन अक्सर इसके कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में, धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए केवल सतही पाठ नहीं, बल्कि इसके गहरे दार्शनिक और तात्कालिक सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों का सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक है। यह हमें मनुस्मृति के उन शाश्वत सिद्धांतों तक पहुँचने में मदद करेगा जो धर्म को केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि कर्तव्य, नैतिकता और सामंजस्यपूर्ण जीवन-शैली के रूप में परिभाषित करते हैं।

धर्म: केवल पंथ नहीं, जीवन का सार
जब हम ‘धर्म’ शब्द सुनते हैं, तो अक्सर हमारे मन में किसी विशेष पंथ या मजहब की छवि उभरती है। लेकिन भारतीय दर्शन में, विशेषकर प्राचीन ग्रंथों में, धर्म का अर्थ कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। यह केवल पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है, एक नैतिक संहिता है जो व्यक्ति और समाज को सही दिशा में ले जाती है। धर्म का वास्तविक अर्थ है ‘धारण करना’ – वह सब कुछ जिसे धारण करने से समाज और व्यक्ति का कल्याण हो, जो जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। इसमें कर्तव्य, नैतिकता, सदाचार, न्याय और उन सार्वभौमिक सिद्धांतों का समावेश है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं। यह व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव और उसके बाहरी आचरण का संतुलन है, जो उसे सही और गलत के बीच भेद करने में मदद करता है।
मनुस्मृति: एक प्राचीन पथप्रदर्शक का परिचय
प्राचीन भारतीय साहित्य में ‘मनुस्मृति’ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रंथ है। इसे अक्सर ‘मानव धर्मशास्त्र’ या ‘मनु संहिता’ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा प्राचीन पाठ है जिसे परंपरा के अनुसार ऋषि मनु द्वारा संकलित किया गया माना जाता है। मनुस्मृति में तत्कालीन समाज के लिए नैतिक, सामाजिक, कानूनी और धार्मिक नियमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह उस समय के सामाजिक ताने-बाने, वर्ण व्यवस्था, पारिवारिक संबंधों, राजा के कर्तव्यों, न्याय प्रणाली और व्यक्तिगत आचरण से जुड़े दिशानिर्देशों का एक संग्रह है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति को लेकर विभिन्न व्याख्याएं और विवाद भी रहे हैं, खासकर आधुनिक संदर्भ में। हालांकि, इसके मूल सिद्धांतों और नैतिक उपदेशों का अध्ययन हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद कर सकता है, बशर्ते हम इसे इसके ऐतिहासिक संदर्भ और विभिन्न दृष्टिकोणों से समझें। इस ग्रंथ का अध्ययन करते समय, हमें इसके शाश्वत सिद्धांतों को समय-विशेष की परिस्थितियों से अलग करके देखने की क्षमता विकसित करनी होगी।
मनुस्मृति में वर्णित धर्म के मूल स्तंभ: दश धर्म लक्षण
मनुस्मृति में धर्म के दस महत्वपूर्ण लक्षण (दश धर्म लक्षण) बताए गए हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए सदाचारी जीवन जीने के लिए आधारशिला का काम करते हैं। ये लक्षण केवल धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े नहीं हैं, बल्कि ये मानव व्यवहार और आंतरिक गुणों पर केंद्रित हैं। ये हमें धर्म के सार्वभौमिक और कालातीत स्वरूप को समझने में मदद करते हैं:
- धृति (धैर्य): किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना, मुश्किलों में भी विचलित न होना। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है।
- क्षमा (क्षमाशीलता): दूसरों की गलतियों को माफ करना और बदले की भावना न रखना। यह आंतरिक शांति और रिश्तों में सामंजस्य लाता है।
- दम (मन पर नियंत्रण): अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना, विशेष रूप से अनुचित प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना। यह आत्म-अनुशासन का प्रतीक है।
- अस्तेय (चोरी न करना): किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना न लेना। यह ईमानदारी और नैतिकता का मूलभूत सिद्धांत है।
- शौच (पवित्रता): शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर शुद्धता बनाए रखना। इसमें स्वच्छता, विचारों की पवित्रता और इरादों की स्पष्टता शामिल है।
- इंद्रियनिग्रह (इंद्रियों पर नियंत्रण): अपनी इंद्रियों (देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना) को अनियंत्रित होने से रोकना। यह हमें बाहरी प्रलोभनों से बचाता है।
- धी (बुद्धि): सही और गलत के बीच विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता। यह ज्ञान और समझ का उपयोग कर जीवन के मार्ग को आलोकित करती है।
- विद्या (ज्ञान): आत्म-ज्ञान और लौकिक ज्ञान दोनों की प्राप्ति। यह अज्ञानता को दूर कर सत्य की ओर ले जाती है।
- सत्य (सत्यवादिता): हमेशा सच बोलना और अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में ईमानदारी बनाए रखना। यह विश्वास और विश्वसनीयता का आधार है।
- अक्रोध (क्रोध न करना): क्रोध और प्रतिशोध की भावनाओं से दूर रहना। यह मानसिक शांति और दूसरों के प्रति सद्भाव को बढ़ावा देता है।
ये ‘दश धर्म लक्षण’ बताते हैं कि मनुस्मृति केवल कर्मकांडों या सामाजिक नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मानव चरित्र के उत्थान और एक सुव्यवस्थित समाज के निर्माण पर जोर देती है। ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन काल में थे।
वर्णधर्म और आश्रमधर्म: समाज और व्यक्ति का संतुलन
मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए ‘वर्णधर्म’ और ‘आश्रमधर्म’ की अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन इनके मूल में समाज और व्यक्ति के बीच संतुलन और कर्तव्यों का विभाजन निहित है।
- वर्णधर्म: मूल रूप से, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर गुणों और कर्मों पर आधारित थी। इसका उद्देश्य समाज में कार्यों का कुशल विभाजन करना था ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति और योग्यता के अनुसार योगदान दे सके। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त करने और दूसरों को शिक्षित करने की प्रवृत्ति है, तो उसका ‘वर्ण’ ब्राह्मण हो सकता है। यदि किसी में रक्षा और नेतृत्व के गुण हैं, तो क्षत्रिय। व्यापार और कृषि के लिए वैश्य, और सेवा कार्यों के लिए शूद्र। इस प्रकार, यह अवधारणा सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और प्रत्येक व्यक्ति को समाज में एक उपयोगी भूमिका प्रदान करने के लिए थी। हालाँकि, समय के साथ इसमें विकृतियाँ आईं और यह जन्म आधारित कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई, जिससे कई सामाजिक असमानताएँ उत्पन्न हुईं। मनुस्मृति के गहन अध्ययन में, हमें इसके मूल उद्देश्य को समझना होगा, जो कि सामाजिक सद्भाव और कार्यात्मक दक्षता पर आधारित था।
- आश्रमधर्म: यह व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न चरणों और उनसे जुड़े कर्तव्यों को संदर्भित करता है। मनुस्मृति में मानव जीवन को चार प्रमुख आश्रमों में बांटा गया है, प्रत्येक का अपना विशिष्ट उद्देश्य है:
- ब्रह्मचर्य आश्रम: यह जीवन का पहला चरण है, जिसमें छात्र गुरु के सान्निध्य में विद्या अध्ययन और आत्म-अनुशासन का पालन करता है। इसका लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना और चरित्र का निर्माण करना है।
- गृहस्थ आश्रम: यह दूसरा चरण है, जिसमें व्यक्ति विवाह करके परिवार का पालन-पोषण करता है, सामाजिक जिम्मेदारियां निभाता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यह समाज की रीढ़ है।
- वानप्रस्थ आश्रम: यह तीसरा चरण है, जिसमें व्यक्ति पारिवारिक जिम्मेदारियों से धीरे-धीरे मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति और समाज सेवा पर ध्यान केंद्रित करता है।
- संन्यास आश्रम: यह जीवन का अंतिम चरण है, जिसमें व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों का त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए एकांत में तपस्या और ध्यान करता है।
ये आश्रम व्यक्ति के जीवन को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज और स्वयं के समग्र विकास के लिए है।
मनुस्मृति के शाश्वत सिद्धांत और आज की दुनिया
भले ही मनुस्मृति हजारों साल पहले लिखी गई हो, लेकिन इसके कई सिद्धांत आज भी हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में प्रासंगिक हैं। हमें इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखना चाहिए और इसके उन शाश्वत मूल्यों को निकालना चाहिए जो किसी भी युग में लागू हो सकते हैं।
- नैतिक आचरण का महत्व: ‘दश धर्म लक्षण’ (धैर्य, क्षमा, सत्य, अक्रोध आदि) आज भी एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन के लिए आधारभूत हैं। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर ईमानदारी (अस्तेय) और सहकर्मियों के प्रति धैर्य (धृति) न केवल व्यक्तिगत सफलता बल्कि एक सकारात्मक कार्य संस्कृति के लिए भी आवश्यक हैं।
- आत्म-नियंत्रण और संतुलन: इंद्रियों पर नियंत्रण (इंद्रियनिग्रह) हमें आज के डिजिटल युग में अति-उत्तेजना और अनावश्यक भोग से बचाता है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बचना या अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना इसके आधुनिक अनुप्रयोग हैं।
- सामाजिक जिम्मेदारी: आश्रमधर्म की अवधारणा हमें सिखाती है कि जीवन के हर चरण में हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। गृहस्थ आश्रम के सिद्धांत आज भी परिवार और समाज के प्रति हमारी भूमिका को परिभाषित करते हैं – बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों का सम्मान, और सामुदायिक कल्याण में योगदान।
- न्याय और निष्पक्षता: मनुस्मृति में राजा के कर्तव्यों और न्याय प्रणाली पर बल दिया गया है, जो आज भी सुशासन और कानून के शासन के महत्व को रेखांकित करता है। यद्यपि उसकी दंड संहिता आज के मानदंडों से भिन्न हो सकती है, न्याय प्रदान करने का मूल सिद्धांत अपरिवर्तित है।
- पर्यावरण चेतना: यद्यपि मनुस्मृति में सीधे तौर पर ‘पर्यावरण’ शब्द का प्रयोग नहीं है, इसके कई श्लोक प्रकृति के प्रति सम्मान और उसके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल देते हैं, जो आज के सतत विकास के सिद्धांतों से मेल खाते हैं।
उदाहरण के लिए, मेरी अपनी यात्रा में, मैंने पाया है कि जब मैंने अपने करियर में चुनौतियों का सामना किया, तो मनुस्मृति में वर्णित ‘धैर्य’ (धृति) के सिद्धांत ने मुझे हार न मानने और समाधान खोजने में मदद की। इसी तरह, जब मैंने अपनी टीम में संघर्षों का सामना किया, तो ‘क्षमा’ और ‘अक्रोध’ के सिद्धांतों ने मुझे विवादों को रचनात्मक रूप से हल करने और संबंधों को बनाए रखने में सक्षम बनाया। ये सिद्धांत केवल किताबी नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में लागू करने योग्य हैं।
मनुस्मृति को समझने की सही दृष्टि
मनुस्मृति को समझना एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें केवल शाब्दिक अर्थों से परे देखना शामिल है। इसे समझने के लिए एक संतुलित और आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है:
- ऐतिहासिक संदर्भ को समझें: मनुस्मृति उस समय के समाज और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप लिखी गई थी। उस काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ आज से बहुत भिन्न थीं। कुछ नियम जो उस समय प्रासंगिक थे, आज अनुपयुक्त लग सकते हैं। उन्हें उस संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए, न कि वर्तमान के चश्मे से।
- सार्वभौमिक सिद्धांतों पर ध्यान दें: जैसा कि ऊपर चर्चा की गई, ‘दश धर्म लक्षण’ जैसे सिद्धांत सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं। वे किसी भी समय और किसी भी समाज में लागू हो सकते हैं। हमें इन्हीं शाश्वत मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मानव नैतिकता और कल्याण को बढ़ावा देते हैं।
- व्याख्याओं की बहुलता: मनुस्मृति की कई टीकाएँ और व्याख्याएँ हैं। अलग-अलग विद्वानों ने इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। किसी एक व्याख्या पर निर्भर रहने के बजाय, विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करना हमें एक व्यापक समझ विकसित करने में मदद करता है।
- आंतरिक भावना बनाम शाब्दिक अर्थ: कभी-कभी, प्राचीन ग्रंथों में दिए गए निर्देश प्रतीकात्मक या रूपकात्मक होते हैं। मनुस्मृति के कुछ अंशों को उनकी आंतरिक भावना के आधार पर समझना चाहिए, न कि केवल उनके शाब्दिक अर्थ के आधार पर। उदाहरण के लिए, कुछ कठोर दंड विधानों को उस समय की न्यायिक प्रणाली और अपराधों की रोकथाम के तरीकों के रूप में देखा जा सकता है, न कि आज के संदर्भ में सीधे लागू करने के लिए।
- आलोचनात्मक विश्लेषण: किसी भी प्राचीन ग्रंथ की तरह, मनुस्मृति का भी आलोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे खारिज कर दिया जाए, बल्कि इसके उन पहलुओं पर विचार किया जाए जो आज के नैतिक और मानवाधिकार मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं। एक परिपक्व पाठक वह होता है जो ज्ञान को ग्रहण करता है लेकिन विवेक से उसका मूल्यांकन भी करता है।
वास्तव में, मनुस्मृति का ज्ञान हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने में तब ही मदद कर सकता है, जब हम इसे एक ऐतिहासिक और दार्शनिक दस्तावेज के रूप में देखें, जिसके कुछ अंशों में कालातीत ज्ञान है और कुछ अंश समय-विशेष की उपज हैं। यह हमें अपनी नैतिक समझ को गहरा करने और एक अधिक जिम्मेदार व्यक्ति बनने में सहायक हो सकता है।
निष्कर्ष
धर्म का वास्तविक स्वरूप केवल प्राचीन ग्रंथों के शाब्दिक अर्थों में नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने और वर्तमान संदर्भ में समझने में निहित है। मनुस्मृति का ज्ञान हमें एक दर्पण दिखाता है, जहाँ हम अपने कर्मों, विचारों और इंद्रियों पर नियंत्रण की आवश्यकता को पहचानते हैं। आज के डिजिटल युग में, जहाँ सूचनाओं की बाढ़ है, सत्यनिष्ठा (अस्तेय का व्यापक रूप) और आत्म-नियंत्रण (इंद्रियों पर संयम) जैसे मनुस्मृति के सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। मैंने स्वयं पाया है कि जब हम क्रोध या निराशा के क्षणों में क्षमा के महत्व को समझते हैं, या दिखावे की बजाय आंतरिक पवित्रता पर ध्यान देते हैं, तो जीवन में एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि धर्म के सार को जीना है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप मनुस्मृति के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें जो सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, और आत्म-अनुशासन की बात करते हैं। इन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करें – चाहे वह सोशल मीडिया पर सोच-समझकर बोलना हो या अपने समय का सदुपयोग करना। यह एक सतत आध्यात्मिक यात्रा है, जहाँ प्रत्येक दिन धर्म के एक नए आयाम को खोजने का अवसर मिलता है। इस ज्ञान को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि जिएँ और एक अधिक संतुलित, सार्थक जीवन की ओर अग्रसर हों।
More Articles
अस्तेय क्या है मनुस्मृति के अनुसार
मनुस्मृति में क्षमा का महत्व
इंद्रियों और मन को वश में कैसे रखें मनुस्मृति के उपाय
वैदिक धर्म क्या है जानें मनुस्मृति से इसके मूल सिद्धांत
कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध मनुस्मृति से समझेंFAQs
धर्म का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए मनुस्मृति का अध्ययन क्यों आवश्यक है?
मनुस्मृति प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण धर्मग्रंथ है जो धर्म के सिद्धांतों, कर्तव्यों, सामाजिक व्यवस्था और नैतिक आचरण का विस्तृत वर्णन करता है। यह धर्म को केवल कर्मकांड तक सीमित न रखकर व्यक्तिगत, सामाजिक और राजधर्म के व्यापक पहलुओं को समझाता है, जिससे धर्म की गहरी और समग्र समझ विकसित होती है।
मनुस्मृति के अनुसार धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं?
मनुस्मृति धर्म के दस लक्षणों का उल्लेख करती है: धृति (धैर्य), क्षमा (क्षमाशीलता), दम (इंद्रिय-निग्रह), अस्तेय (चोरी न करना), शौच (पवित्रता), इंद्रिय-निग्रह (इंद्रियों पर नियंत्रण), धी (बुद्धि), विद्या (ज्ञान), सत्य (सच्चाई) और अक्रोध (क्रोधहीनता)। ये सिद्धांत व्यक्ति को नैतिक और धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।
क्या मनुस्मृति में वर्णित धर्म आज के आधुनिक समाज में प्रासंगिक है?
मनुस्मृति के कुछ नियम काल और समाज के अनुसार बदलते प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन इसके मूल नैतिक और सार्वभौमिक सिद्धांत – जैसे सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना – आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमें इसके मूल संदेश को समझना चाहिए, न कि केवल शाब्दिक व्याख्या पर जोर देना चाहिए।
मनुस्मृति धर्म को केवल कर्मकांड या पूजा-पाठ से अलग कैसे परिभाषित करती है?
मनुस्मृति के अनुसार, धर्म केवल पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह व्यक्ति के आचरण, कर्तव्य, नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और जीवन के हर पहलू में न्यायसंगत व्यवहार को समाहित करता है। इसमें वर्ण-धर्म, आश्रम-धर्म, राजधर्म और सामान्य धर्म (सार्वभौमिक नैतिकता) सभी शामिल हैं, जो एक व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखते हैं।
मनुस्मृति में ‘स्वधर्म’ की अवधारणा का क्या महत्व है?
मनुस्मृति ‘स्वधर्म’ पर विशेष बल देती है, जिसका अर्थ है अपने वर्ण, आश्रम और स्थिति के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। यह अवधारणा व्यक्ति को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने में मदद करती है, जिससे समाज में व्यवस्था और संतुलन बना रहता है। स्वधर्म का पालन करना ही परम धर्म माना गया है।
क्या मनुस्मृति में धर्म की कुछ ऐसी व्याख्याएं हैं जिन पर विवाद होता रहा है?
हाँ, मनुस्मृति के कुछ श्लोकों, विशेषकर जो वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति और दंड विधान से संबंधित हैं, पर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में काफी विवाद रहा है। इन विवादों का कारण अक्सर श्लोकों की शाब्दिक व्याख्या और उनके ऐतिहासिक संदर्भ को समझने में अंतर होता है। विद्वानों का मत है कि ग्रंथ को उसके पूरे संदर्भ और समय काल के अनुसार देखना महत्वपूर्ण है।
मनुस्मृति के ज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को कैसे अपना सकता है?
मनुस्मृति के ज्ञान से व्यक्ति धैर्य, क्षमा, आत्म-नियंत्रण, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता जैसे नैतिक मूल्यों को सीख सकता है। यह उसे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है, न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए प्रेरित करता है और एक संतुलित तथा धर्मनिष्ठ जीवन जीने की दिशा प्रदान करता है।