भारत में गरीबी की समझ अब केवल आय के आंकड़ों तक सीमित नहीं रही है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) रिपोर्ट 2023 के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में लाखों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो इस बात का संकेत है कि अब हम पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे मानव निर्धनता के विविध आयामों को अधिक गंभीरता से देख रहे हैं। यह बदलाव, जहां एक ओर प्रगति दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट करता है कि वास्तविक विकास तभी संभव है जब हम हर व्यक्ति को बुनियादी गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर प्रदान करें, न कि सिर्फ उसे न्यूनतम आय के दायरे में बांधें। यह नई परिभाषा हमें गरीबी उन्मूलन के लिए अधिक समग्र और प्रभावी नीतियां बनाने की दिशा में प्रेरित करती है।
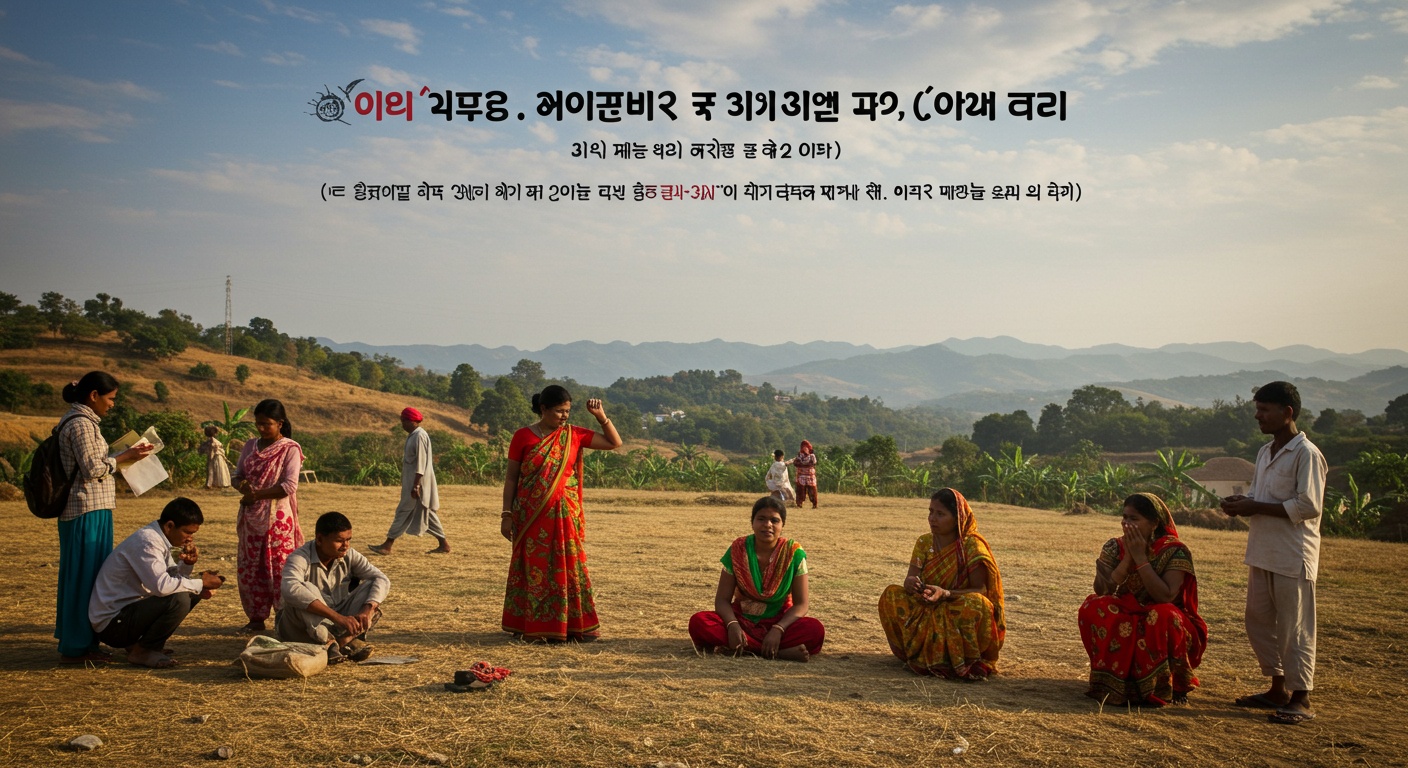
गरीबी: एक बदलती हुई अवधारणा
भारत में गरीबी की परिभाषा समय के साथ लगातार विकसित हुई है। दशकों पहले, गरीबी को मुख्य रूप से आय या उपभोग के स्तर के आधार पर देखा जाता था। इसका मतलब था कि यदि किसी व्यक्ति या परिवार की आय एक निश्चित ‘गरीबी रेखा’ से नीचे है, तो उसे गरीब माना जाता था। यह गरीबी रेखा आमतौर पर न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक खर्च पर आधारित होती थी। इसे ‘आय गरीबी’ या ‘परंपरागत गरीबी’ के रूप में जाना जाता है।
उदाहरण के लिए, 1970 और 80 के दशक में, गरीबी का आकलन मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित था कि क्या लोग अपनी बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। लेकिन, जैसे-जैसे समाज और अर्थव्यवस्था जटिल होती गई, यह महसूस किया गया कि केवल आय या कैलोरी सेवन गरीबी का पूरा चित्र प्रस्तुत नहीं करते। एक व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन हो सकता है, लेकिन यदि उसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या स्वच्छ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच नहीं मिलती, तो क्या वह वास्तव में गरीब नहीं है?
धीरे-धीरे, इस पारंपरिक दृष्टिकोण में बदलाव आया और विशेषज्ञों ने गरीबी को एक बहुआयामी घटना के रूप में देखना शुरू किया। यह बदलाव कक्षा 9 अर्थशास्त्र में भी पढ़ाया जाता है, जहाँ छात्रों को गरीबी के विभिन्न आयामों से परिचित कराया जाता है।
बहुआयामी गरीबी: एक व्यापक दृष्टिकोण
आधुनिक समय में, गरीबी को केवल आय की कमी के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि इसे कई अभावों के योग के रूप में समझा जाता है। इसे ‘बहुआयामी गरीबी’ (Multidimensional Poverty) कहते हैं। यह अवधारणा मानती है कि गरीब होने का मतलब केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा से वंचित होना, पीने के साफ पानी का अभाव, बिजली की अनुपलब्धता, और स्वच्छता की कमी भी शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफ़ोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा विकसित बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) इस दृष्टिकोण का एक प्रमुख उदाहरण है। यह सूचकांक तीन मुख्य आयामों और दस संकेतकों पर आधारित है:
- स्वास्थ्य:
- पोषण (Nutrition)
- बाल मृत्यु दर (Child Mortality)
- शिक्षा:
- स्कूली शिक्षा के वर्ष (Years of Schooling)
- स्कूल में उपस्थिति (School Attendance)
- जीवन स्तर:
- खाना पकाने का ईंधन (Cooking Fuel)
- स्वच्छता (Sanitation)
- पीने का पानी (Drinking Water)
- बिजली (Electricity)
- आवास (Housing)
- संपत्ति (Assets)
यदि कोई व्यक्ति इन दस संकेतकों में से एक तिहाई या उससे अधिक में वंचित पाया जाता है, तो उसे बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है। भारत में नीति आयोग भी MPI का उपयोग करके गरीबी का आकलन करता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई कहाँ तक पहुंची है और किन क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
आय गरीबी बनाम बहुआयामी गरीबी
इन दोनों अवधारणाओं के बीच का अंतर समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नीतियों और हस्तक्षेपों के डिजाइन को प्रभावित करता है।
| विशेषता | आय गरीबी (परंपरागत दृष्टिकोण) | बहुआयामी गरीबी (आधुनिक दृष्टिकोण) |
|---|---|---|
| परिभाषा का आधार | न्यूनतम आय या उपभोग व्यय। | स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभावों का संयोजन। |
| माप का तरीका | एकल मौद्रिक रेखा (गरीबी रेखा)। | कई संकेतक और आयाम (जैसे MPI)। |
| फोकस | आर्थिक अभाव। | मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में अभाव। |
| नीतिगत निहितार्थ | आय-हस्तांतरण योजनाएं, सब्सिडी। | एकीकृत विकास कार्यक्रम, बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान। |
| उदाहरण | राशन कार्ड, मनरेगा (शुरुआती चरण)। | स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, हर घर जल। |
एक वास्तविक जीवन का उदाहरण लें: एक दिहाड़ी मजदूर जिसकी आय गरीबी रेखा से ऊपर है, लेकिन उसके पास शौचालय नहीं है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, और उसके घर में बिजली नहीं है। आय गरीबी के अनुसार वह गरीब नहीं है, लेकिन बहुआयामी गरीबी के अनुसार वह गंभीर रूप से गरीब है। यह दिखाता है कि हमें केवल आय पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन की समग्र गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
मानव निर्धनता: एक गहरी समझ
बहुआयामी गरीबी का विस्तार ही ‘मानव निर्धनता’ (Human Poverty) की अवधारणा है। यह केवल अभावों को मापने से एक कदम आगे है, यह इस बात पर जोर देती है कि गरीबी का मतलब सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि मानव क्षमताओं और अवसरों की कमी भी है। मानव निर्धनता सूचकांक (Human Poverty Index – HPI), जिसे UNDP ने विकसित किया था (अब MPI ने इसका स्थान ले लिया है), जीवन के तीन मुख्य क्षेत्रों में अभावों को मापता था:
- लंबा और स्वस्थ जीवन जीना: जन्म के समय कम जीवन प्रत्याशा।
- ज्ञान प्राप्त करना: वयस्क निरक्षरता दर।
- एक सम्मानजनक जीवन स्तर: पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और बच्चों के कम वजन का प्रतिशत।
मानव निर्धनता का महत्व इस बात पर है कि यह हमें याद दिलाता है कि गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, बल्कि यह मानव गरिमा, आत्म-सम्मान और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। जब एक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य या सुरक्षित वातावरण नहीं मिलता, तो उसकी क्षमताएं कुंठित हो जाती हैं, और वह समाज में पूरी तरह से योगदान नहीं दे पाता।
कल्पना कीजिए कि एक गाँव की लड़की जो पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन स्कूल दूर होने और परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण उसे अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ती है। यह सिर्फ आय का अभाव नहीं है, यह उसकी क्षमताओं का अभाव है, उसके सपनों का अभाव है। यह मानव निर्धनता का एक दर्दनाक उदाहरण है।
भारत में बदलती परिभाषा के निहितार्थ और कार्रवाई
गरीबी की बदलती परिभाषा ने भारत में नीति निर्माण और विकास कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। अब सरकारें केवल आय सहायता पर ध्यान केंद्रित नहीं करतीं, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती हैं।
- समग्र विकास पर जोर: स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छता), प्रधानमंत्री आवास योजना (आवास), जल जीवन मिशन (पीने का पानी), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (खाना पकाने का ईंधन) जैसी योजनाएं सीधे तौर पर बहुआयामी गरीबी के संकेतकों को संबोधित करती हैं। ये योजनाएं सुनिश्चित करती हैं कि लोगों को सिर्फ आय ही नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाएं भी मिलें जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएं।
- लक्ष्यीकरण में सुधार: बहुआयामी गरीबी के आंकड़े हमें यह समझने में मदद करते हैं कि देश के किन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा या स्वच्छता के मोर्चे पर अधिक काम करने की आवश्यकता है। यह लक्षित हस्तक्षेपों को संभव बनाता है।
- मानव पूंजी में निवेश: शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को अब गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मजबूत मानव पूंजी ही किसी भी देश के दीर्घकालिक विकास का आधार होती है।
- भागीदारी और सशक्तिकरण: जब लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं और उनकी क्षमताओं का विकास होता है, तो वे स्वयं गरीबी से बाहर निकलने में अधिक सक्षम होते हैं। यह उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी अधिक सक्रिय भागीदार बनाता है।
संक्षेप में, भारत में गरीबी की परिभाषा का विकास एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है – एक ऐसा बदलाव जो हमें यह सिखाता है कि हमें सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को गिनना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण और सार्थक जीवन जीने का अवसर मिले। यह सिर्फ आर्थिक समृद्धि का मामला नहीं है, बल्कि मानव सम्मान और अधिकारों की रक्षा का भी है।
निष्कर्ष
भारत में गरीबी की परिभाषा अब केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सम्मान जैसे मानवीय पहलुओं को भी समाहित करती है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्टों से स्पष्ट है कि बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है, जो दर्शाता है कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से महत्वपूर्ण प्रगति संभव है। परंतु, यह समझना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक मानव निर्धनता केवल आंकड़ों से परे है; यह गरिमा, अवसरों और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी है। एक नागरिक के तौर पर, हमें अपने आसपास शिक्षा, कौशल विकास और जागरूकता फैलाने में योगदान देना चाहिए। मुझे लगता है कि जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी बच्चे की शिक्षा या किसी युवा के कौशल विकास में छोटा सा भी सहयोग करते हैं, तो हम गरीबी के इस दुष्चक्र को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सिर्फ सरकारी योजनाओं का काम नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए, एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहाँ हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने का अवसर मिले और कोई भी मानवीय निर्धनता से ग्रसित न हो।
अधिक लेख
बहुआयामी गरीबी क्या है? इसके 12 मुख्य संकेतक जो जीवन स्तर का खुलासा करते हैं
भारत में निर्धनता उन्मूलन सरकारी योजनाएँ और उनके प्रभाव
मानव पूंजी का महत्व और भारत में रोजगार के अवसर
भारत में गरीबी का मापन कैसे होता है? कैलोरी और बहुआयामी सूचकांक को समझें
गरीबी के बहुआयामी रूप और प्रमुख कारण समझें
FAQs
भारत में गरीबी की पारंपरिक परिभाषा क्या रही है?
पारंपरिक रूप से, भारत में गरीबी को मुख्य रूप से आय या उपभोग के स्तर के आधार पर परिभाषित किया जाता रहा है। इसमें एक निश्चित “गरीबी रेखा” निर्धारित की जाती थी, जो व्यक्ति के न्यूनतम कैलोरी सेवन या आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने की क्षमता पर आधारित होती थी।
हाल के वर्षों में भारत में गरीबी की परिभाषा में क्या बदलाव आया है?
हाल के वर्षों में, भारत में गरीबी की परिभाषा आय-आधारित दृष्टिकोण से हटकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण की ओर बढ़ी है। अब इसमें केवल धन की कमी नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, स्वच्छता, पीने का पानी और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का अभाव भी शामिल है। यह बदलाव मानव विकास और क्षमताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
“मानव निर्धनता” से क्या अभिप्राय है और इसका महत्व क्यों बढ़ गया है?
मानव निर्धनता का अर्थ केवल धन की कमी नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में विकल्पों, अवसरों और क्षमताओं के अभाव से है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होना, शिक्षा से वंचित रहना, गरिमापूर्ण जीवन जीने में अक्षमता और सामाजिक बहिष्कार शामिल हैं। इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यह गरीबी के गहरे और व्यापक पहलुओं को उजागर करती है, जो केवल आर्थिक आंकड़ों से परे होते हैं।
भारत में मानव निर्धनता को मापने के लिए किन मापदंडों का उपयोग किया जाता है?
भारत में मानव निर्धनता को मापने के लिए अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index – MPI) का उपयोग किया जाता है। नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया यह सूचकांक तीन प्रमुख आयामों – स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर – पर आधारित है, जिनमें पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और संपत्ति जैसे 12 संकेतक शामिल हैं।
आय गरीबी और मानव निर्धनता में मुख्य अंतर क्या है?
आय गरीबी मुख्य रूप से एक व्यक्ति या परिवार की वित्तीय क्षमता पर केंद्रित होती है, यानी उनके पास आय कितनी है या वे कितना खर्च कर सकते हैं। इसके विपरीत, मानव निर्धनता एक व्यापक अवधारणा है जो जीवन की गुणवत्ता, बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच, अवसरों और क्षमताओं के अभाव को दर्शाती है। यह धन की कमी के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और गरिमा जैसे अमूर्त पहलुओं को भी शामिल करती है।
नीति निर्माण में मानव निर्धनता के महत्व को समझना क्यों आवश्यक है?
नीति निर्माण में मानव निर्धनता के महत्व को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह सरकारों को गरीबी के मूल कारणों को संबोधित करने और अधिक लक्षित तथा प्रभावी नीतियां बनाने में मदद करता है। यह केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, मानव विकास, सामाजिक न्याय और समावेशी वृद्धि को प्राथमिकता देता है, जिससे दीर्घकालिक और स्थायी समाधान प्राप्त हो सकें।
भारत में मानव निर्धनता को संबोधित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
भारत सरकार मानव निर्धनता को संबोधित करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। इनमें पोषण अभियान (स्वास्थ्य), सर्व शिक्षा अभियान और नई शिक्षा नीति (शिक्षा), स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छता), प्रधानमंत्री आवास योजना (आवास), उज्ज्वला योजना (खाना पकाने का ईंधन), जल जीवन मिशन (पेयजल) और आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य सेवाएं) शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य विभिन्न आयामों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।










