आधुनिक जीवन की जटिलताएँ और त्वरित निर्णय अक्सर हमें अनजाने में ऐसे कर्मों के जाल में फँसा देते हैं, जिनके सूक्ष्म प्रभाव ‘संस्कार’ बनकर हमारी चेतना पर अंकित हो जाते हैं। पर्यावरणीय असंतुलन से लेकर व्यक्तिगत संबंधों में तनाव तक, हमारे प्रत्येक कार्य का परिणाम अंततः हमें ही भोगना पड़ता है। ऐसे में, वैदिक ज्ञान केवल अनुष्ठानों का संग्रह नहीं, बल्कि कर्मों के मूल स्वभाव, उनके दोषों की पहचान और उन्हें शुद्ध करने का एक गहन विज्ञान प्रस्तुत करता है। यह हमें अज्ञानजनित क्रियाओं के चक्र को समझने, नकारात्मक प्रभावों को ‘प्रायश्चित्त’ और ‘आत्म-ज्ञान’ के माध्यम से निर्मल करने का मार्ग दिखाता है, जिससे हम कर्मों के फल से मुक्ति पाकर एक संतुलित व सचेत जीवन जी सकें। यह प्राचीन विद्या आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी हजारों साल पहले थी।
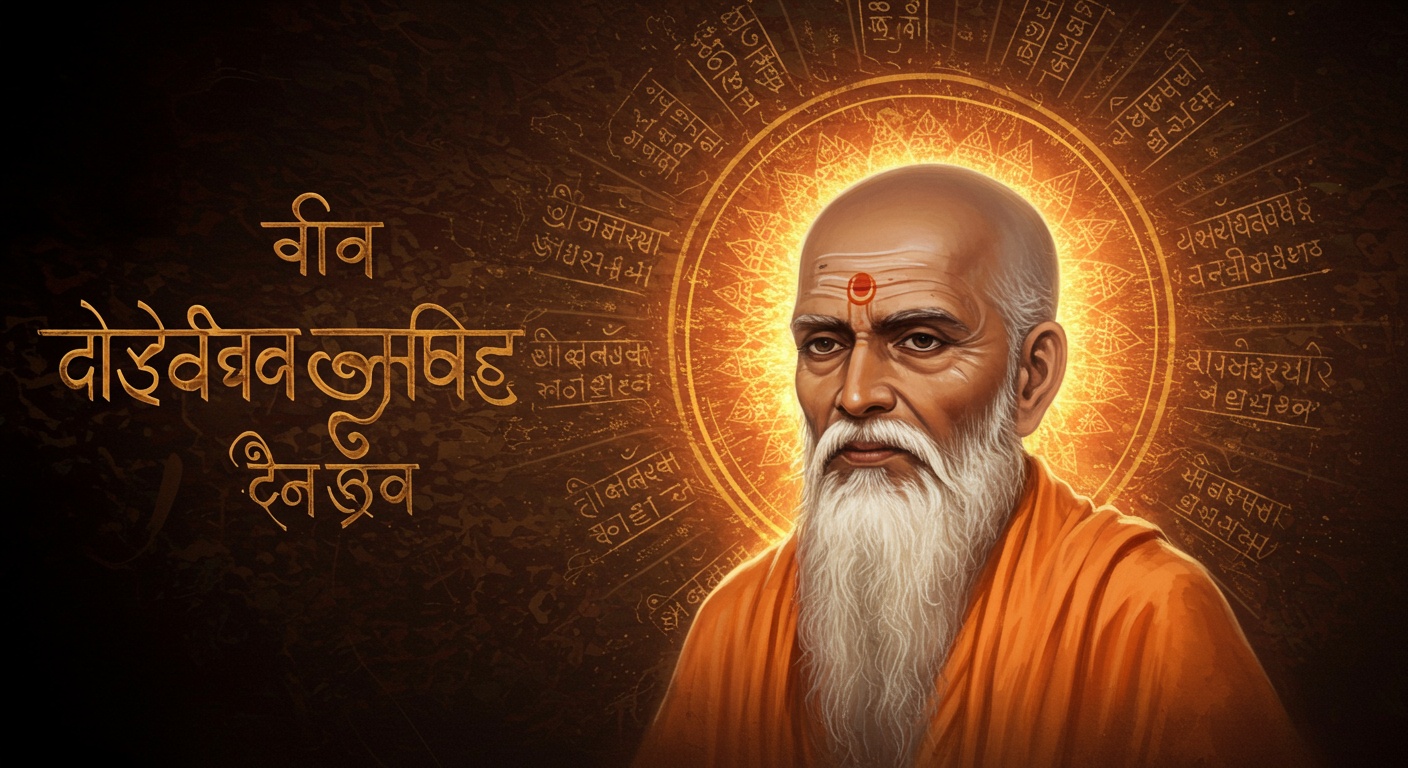
कर्म और उसके दोषों को समझना
कर्म, जिसे हम अक्सर केवल ‘कार्य’ समझते हैं, वैदिक परंपरा में इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है। यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और इरादों का भी समुच्चय है। हर कर्म, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, एक निश्चित परिणाम उत्पन्न करता है, जिसे हम ‘कर्म फल’ कहते हैं। यह कर्म फल ही हमारे वर्तमान और भविष्य के अनुभवों को आकार देता है।
कर्म मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं:
- संचित कर्म: यह हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के उन सभी कर्मों का संग्रह है जिनके फल अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं। यह एक विशाल बैंक खाते की तरह है जिसमें हमारे सभी कर्मों का लेखा-जोखा जमा है।
- प्रारब्ध कर्म: यह संचित कर्मों का वह हिस्सा है जो इस वर्तमान जीवन में फल देने के लिए परिपक्व हो चुका है। यह वह भाग्य है जिसे हम इस जन्म में अनुभव करते हैं, और इससे बचना असंभव है, हालांकि इसके प्रभावों को नरम किया जा सकता है।
- क्रियमाण कर्म: यह वे कर्म हैं जो हम वर्तमान क्षण में कर रहे हैं। इन कर्मों का फल तुरंत या भविष्य में प्राप्त होता है, और यही वह क्षेत्र है जहाँ हमारे पास सबसे अधिक स्वतंत्रता और नियंत्रण होता है। हमारे क्रियमाण कर्म ही हमारे संचित कर्मों के खाते को बढ़ाते या घटाते हैं।
अब बात करते हैं ‘कर्मों के दोषों’ की। कर्मों के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब हम अज्ञानता, अहंकार, राग, द्वेष या मोह से प्रेरित होकर ऐसे कर्म करते हैं जो धर्म के सिद्धांतों के विपरीत होते हैं। ये दोष हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक अशांति और बाहरी जीवन में बाधाओं के रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना या झूठ बोलना कर्म दोष उत्पन्न करता है, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में हमें भी उसी तरह की पीड़ा या अविश्वास का सामना करना पड़ सकता है। ये दोष हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा बनते हैं और हमें बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्र में फँसाए रखते हैं।
वैदिक ज्ञान का सार: मार्ग और प्रकाश
वैदिक ज्ञान, जिसमें वेद, उपनिषद, भगवद गीता और विभिन्न स्मृतियाँ (जैसे मनुस्मृति) शामिल हैं, भारतीय दर्शन का आधार स्तंभ है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने के एक समग्र विज्ञान को प्रस्तुत करता है। इसका मूल उद्देश्य मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से अवगत कराना, उसे धर्म के मार्ग पर चलाना और अंततः मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करना है।
वैदिक ज्ञान हमें बताता है कि हम केवल यह शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा (आत्मा या ब्रह्म) हैं, जो परम चेतना का अंश है। यह ज्ञान हमें संसार की क्षणभंगुरता और कर्मों के अटल नियम को समझने में मदद करता है। वैदिक ऋषि-मुनियों ने गहन तपस्या और ध्यान के माध्यम से इस ज्ञान को प्राप्त किया और इसे मानव कल्याण के लिए संकलित किया।
वैदिक ज्ञान का सार ‘धर्म’ में निहित है। धर्म का अर्थ केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि वह शाश्वत नियम है जो ब्रह्मांड को संतुलित रखता है और मानव समाज को सही दिशा देता है। इसमें नैतिकता, कर्तव्यपरायणता, सत्यनिष्ठा, अहिंसा और सभी जीवों के प्रति करुणा जैसे सिद्धांत शामिल हैं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में धर्म के विस्तृत आयामों और व्यक्ति के कर्तव्यों पर गहन प्रकाश डाला गया है, जिससे समाज में व्यवस्था और न्याय स्थापित हो सके। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे सही कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और कर्मों के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं।
कर्मों के दोषों को दूर करने के वैदिक मार्ग
वैदिक परंपरा में कर्मों के दोषों को दूर करने के कई प्रभावी मार्ग बताए गए हैं। ये मार्ग एक-दूसरे के पूरक हैं और व्यक्ति की प्रकृति तथा आध्यात्मिक झुकाव के अनुसार अपनाए जा सकते हैं।
1. ज्ञान मार्ग (ज्ञान योग)
ज्ञान मार्ग आत्म-साक्षात्कार और परम सत्य की समझ पर आधारित है। यह हमें अज्ञानता से मुक्ति दिलाता है, जो सभी कर्म दोषों का मूल कारण है। जब हमें यह बोध होता है कि हम शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हैं और सभी जीव एक ही परम चेतना के अंश हैं, तो हमारे भीतर से अहंकार और द्वेष समाप्त हो जाते हैं।
- शास्त्र अध्ययन: वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन। यह हमें जीवन के गहरे अर्थ, कर्मों के नियम और मुक्ति के मार्ग को समझने में मदद करता है।
- सत्संग: ज्ञानी गुरुओं और विद्वानों के साथ बैठकर ज्ञान चर्चा करना। यह हमारी शंकाओं को दूर करता है और हमें सही दिशा दिखाता है।
- आत्म-चिंतन: स्वयं के भीतर गहराई से झाँकना, अपनी वृत्तियों, इच्छाओं और प्रेरणाओं का विश्लेषण करना।
उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो पहले केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करता था, ज्ञान मार्ग पर चलकर यह समझता है कि उसका अस्तित्व ब्रह्मांड के एक बड़े हिस्से का हिस्सा है। यह समझ उसे परोपकार और निःस्वार्थ सेवा की ओर ले जाती है, जिससे उसके पुराने कर्मों के दोष क्षीण होने लगते हैं।
2. कर्म मार्ग (निष्काम कर्म योग)
भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया है, जिसका अर्थ है फल की इच्छा के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना। यह मार्ग हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और उनके परिणामों से विरक्त रहते हैं, तो वे कर्म हमारे लिए नए दोष उत्पन्न नहीं करते।
- कर्तव्यपरायणता: अपने वर्ण, आश्रम और स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। मनुस्मृति में विभिन्न वर्णों और आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) के लिए निर्धारित कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिनका पालन व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर स्थिर रखता है और कर्म दोषों से बचाता है।
- सेवा: निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना। यह अहंकार को कम करता है और प्रेम व करुणा को बढ़ाता है।
- अनासक्ति: कर्म फल के प्रति आसक्ति न रखना। यह मन को शांत रखता है और तनाव को कम करता है।
एक उदाहरण के रूप में, एक व्यवसायी जो पहले केवल लाभ के लिए काम करता था, अब अपने व्यवसाय को समाज की सेवा के एक माध्यम के रूप में देखता है। वह ईमानदारी से काम करता है, अपने कर्मचारियों और ग्राहकों का ध्यान रखता है, और लाभ को समाज कल्याण में लगाता है। इस प्रकार किया गया कर्म उसे दोषों से मुक्त करता है।
3. भक्ति मार्ग (भक्ति योग)
भक्ति मार्ग ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम पर आधारित है। यह सबसे सरल और प्रभावी मार्गों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह सीधे हृदय को शुद्ध करता है।
- नाम जप और कीर्तन: ईश्वर के नाम का निरंतर जप करना और संकीर्तन में भाग लेना। यह मन को एकाग्र करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है।
- पूजा और अर्चना: विधि-विधान से देवी-देवताओं की पूजा करना। यह श्रद्धा और समर्पण को बढ़ाता है।
- आत्म-समर्पण: अपनी सभी इच्छाओं, चिंताओं और परिणामों को ईश्वर को समर्पित कर देना। यह हमें मानसिक बोझ से मुक्त करता है।
कई लोगों ने भक्ति मार्ग अपनाकर अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। एक व्यक्ति जो अत्यधिक क्रोधित और चिंतित रहता था, ईश्वर के नाम जप और भक्ति भाव से शांत और आनंदित हो गया, जिससे उसके पुराने नकारात्मक कर्मों का प्रभाव भी कम हुआ।
4. योग मार्ग (अष्टांग योग)
पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक व्यवस्थित तरीका है, जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है।
- यम और नियम: नैतिक आचरण (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) और आत्म-अनुशासन (शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान) का पालन करना। मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र भी इन नैतिक सिद्धांतों पर जोर देते हैं, क्योंकि यही एक शुद्ध जीवन का आधार हैं।
- आसन और प्राणायाम: शारीरिक शुद्धि और ऊर्जा नियंत्रण के लिए योगासन और श्वास अभ्यास।
- ध्यान: मन को एकाग्र करना और आंतरिक शांति प्राप्त करना। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और आत्म-ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कर्म दोषों को जलाने में सहायक है।
नियमित योगाभ्यास और ध्यान से मानसिक शांति मिलती है, जिससे व्यक्ति के निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं और वह अज्ञानवश होने वाले कर्म दोषों से बचता है।
5. प्रायश्चित्त और शुद्धि
वैदिक परंपरा में किए गए कर्म दोषों को दूर करने के लिए ‘प्रायश्चित्त’ का विधान है। प्रायश्चित्त का अर्थ है पश्चाताप, शुद्धि और सकारात्मक कर्मों के माध्यम से किए गए पापों का निराकरण।
- सत्यनिष्ठ पश्चाताप: अपने कर्म दोषों को स्वीकार करना और उनके लिए हृदय से पश्चाताप करना। यह शुद्धि का पहला कदम है।
- दान: ज़रूरतमंदों को दान देना। शास्त्रों में अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान और गौदान को विशेष महत्व दिया गया है। दान से संचित पाप कर्मों का भार कम होता है।
- तपस्या: शारीरिक और मानसिक अनुशासन का पालन करना, जैसे उपवास, मौन व्रत या तीर्थ यात्रा। तपस्या से शरीर और मन शुद्ध होते हैं तथा आत्मिक बल बढ़ता है।
- यज्ञ और होम: वैदिक मंत्रों और अनुष्ठानों के साथ अग्नि में आहुति देना। यज्ञ वातावरण को शुद्ध करते हैं और मन में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं।
- तीर्थ यात्रा: पवित्र स्थानों की यात्रा करना। यह मन को शांत करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है।
मनुस्मृति में विभिन्न प्रकार के पापों और उनके प्रायश्चित्त के विस्तृत नियम दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, अनजाने में किए गए पापों के लिए लघु प्रायश्चित्त और जानबूझकर किए गए गंभीर पापों के लिए कठोर प्रायश्चित्त का विधान है। यह दर्शाता है कि वैदिक ज्ञान न केवल कर्मों को करने के नियम बताता है, बल्कि उनके दोषों को दूर करने का मार्ग भी स्पष्ट करता है। एक व्यक्ति जिसने अतीत में कोई गलत कार्य किया है, वह सच्चे पश्चाताप और प्रायश्चित्त के माध्यम से अपने मन को शुद्ध कर सकता है और नए सकारात्मक कर्मों की नींव रख सकता है।
व्यावहारिक जीवन में वैदिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग
वैदिक ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि अत्यधिक व्यावहारिक है। इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाकर हम कर्मों के दोषों को कम कर सकते हैं और एक संतुलित, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।
यहाँ कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोग दिए गए हैं:
- माइंडफुलनेस और जागरूकता: हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करें। अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं पर ध्यान दें। क्या आप जो कहने या करने वाले हैं, वह किसी को नुकसान पहुँचाएगा? क्या यह सत्य पर आधारित है? यह अभ्यास हमें नकारात्मक कर्म करने से रोकता है।
- नैतिक आचरण: सत्य (सच बोलना), अहिंसा (किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट न देना), अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य (संयम) और अपरिग्रह (आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना) जैसे वैदिक नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। ये यम और नियम हमें धर्म के मार्ग पर स्थिर रखते हैं।
- कृतज्ञता और संतोष: जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। संतोष की भावना विकसित करें। यह अनावश्यक इच्छाओं और लोभ को कम करता है, जो कई कर्म दोषों का कारण बनते हैं।
- क्षमा: दूसरों को क्षमा करना और स्वयं से भी क्षमा माँगना सीखें। मन में द्वेष रखने से नकारात्मक कर्म दोष उत्पन्न होते हैं। क्षमा करने से मन हल्का होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
- नियमित साधना: प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, जप या प्रार्थना के लिए निकालें। यह मन को शांत करता है, आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले की गई साधना विशेष रूप से प्रभावी होती है।
- सात्विक जीवन शैली: सात्विक भोजन (ताजा, पौष्टिक, शाकाहारी) का सेवन करें। स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें। एक स्वस्थ शरीर और मन सकारात्मक कर्मों के लिए एक बेहतर आधार प्रदान करते हैं।
- सेवा भाव: अपने आस-पास के लोगों और समाज के लिए निःस्वार्थ भाव से कुछ करें। छोटे-छोटे कार्य जैसे किसी की मदद करना, किसी को मुस्कुराना या पर्यावरण की रक्षा करना भी पुण्य कर्म माने जाते हैं।
उदाहरण के लिए, एक बार एक व्यक्ति अत्यधिक तनाव और निराशा में था क्योंकि उसे लगता था कि उसके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है। उसने एक आध्यात्मिक गुरु से सलाह ली, जिन्होंने उसे प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान करने, दूसरों की मदद करने और हर बात में कृतज्ञता ढूंढने का सुझाव दिया। कुछ ही हफ्तों में, व्यक्ति ने अपने भीतर एक अद्भुत शांति और सकारात्मकता महसूस की। उसने पाया कि उसकी निराशा कम हो रही है और उसके जीवन में बेहतर अवसर आने लगे हैं। यह दर्शाता है कि कैसे छोटे, सुसंगत वैदिक अभ्यास भी कर्मों के दोषों के प्रभावों को धीरे-धीरे कम कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
निष्कर्ष
वैदिक ज्ञान कर्मों के दोषों को दूर करने का एक शाश्वत मार्ग प्रस्तुत करता है, जो केवल कर्मकांड तक सीमित न होकर हमारी चेतना के गहन रूपांतरण पर केंद्रित है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहाँ अनजाने में भी कई कर्म दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वहाँ आत्म-चिंतन और सही दृष्टिकोण ही हमें इनसे मुक्ति दिला सकता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि सुबह के कुछ पल मौन ध्यान और रात को दिन भर के कार्यों का निष्पक्ष विश्लेषण, हमें अपने भीतर की अशुद्धियों को पहचानने और स्वीकार करने में अद्भुत रूप से मदद करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दोषों से मुक्ति एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें कर्मों की शुद्धि के साथ-साथ सही नियत और दूसरों के प्रति सहानुभूति का विकास भी शामिल है। जैसे आजकल डिजिटल डिटॉक्स का चलन है, वैसे ही हमें अपने मन और विचारों का भी ‘वैदिक डिटॉक्स’ करना चाहिए। अपने इंद्रियों पर संयम रखना और मन को शांत रखना, नए दोषों को उत्पन्न होने से रोकता है। यह सिर्फ पाप से मुक्ति नहीं, बल्कि एक पुण्यमय और संतुष्ट जीवन की नींव है, जो आपको आंतरिक शांति और परम कल्याण की ओर अग्रसर करती है।
More Articles
कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध मनुस्मृति से समझें
मन वाणी और शरीर के पाप कर्मों से कैसे बचें
पाप से मुक्ति के 4 आध्यात्मिक उपाय मनुस्मृति से सीखें
इंद्रियों और मन को वश में कैसे रखें मनुस्मृति के उपाय
मनुस्मृति में क्षमा का महत्व
FAQs
वैदिक ज्ञान क्या है और यह कर्मों से कैसे संबंधित है?
वैदिक ज्ञान प्राचीन भारतीय ग्रंथों, जैसे वेद, उपनिषद, और पुराणों में निहित है। यह जीवन के मौलिक सिद्धांतों, धर्म, अधर्म, कर्म के नियम और मोक्ष के मार्ग को समझाता है। यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कार्य (कर्म) कैसे फल देते हैं और हम अच्छे कर्मों के माध्यम से कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
कर्मों के दोष या ‘कर्म दोष’ क्या होते हैं?
कर्मों के दोष (या कर्म दोष) उन नकारात्मक प्रभावों या परिणामों को संदर्भित करते हैं जो हमारे पिछले या वर्तमान बुरे कार्यों (अधर्मपूर्ण कर्मों) के कारण उत्पन्न होते हैं। ये दोष हमारे जीवन में बाधाओं, दुखों या कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं।
वैदिक ज्ञान की मदद से कर्मों के दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है?
वैदिक ज्ञान कर्मों के दोषों को दूर करने के लिए कई मार्ग सुझाता है। इनमें प्रमुख हैं – धर्मानुसार जीवन जीना, निस्वार्थ भाव से कर्म करना (निष्काम कर्म), ज्ञान प्राप्त करना, तपस्या, दान, यज्ञ, और ईश्वर की भक्ति। सही समझ और आचरण से हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं।
क्या वैदिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ कर्म दोष निवारण में सहायक होते हैं?
हाँ, वैदिक अनुष्ठान, यज्ञ, और पूजा-पाठ कर्म दोष निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्रियाएं मन को शुद्ध करती हैं, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, और देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करती हैं, जिससे नकारात्मक कर्मों के प्रभाव कम होते हैं। हालाँकि, केवल अनुष्ठान ही पर्याप्त नहीं, उनके साथ शुद्ध आचरण और वैराग्य भी आवश्यक है।
निष्काम कर्म का सिद्धांत कर्मों के दोषों को दूर करने में कैसे सहायक है?
निष्काम कर्म का अर्थ है फल की इच्छा के बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। जब हम बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या हानि की चिंता किए कर्म करते हैं, तो हम उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें नए नकारात्मक कर्मों को संचित करने से रोकता है और पिछले कर्मों के प्रभावों को धीरे-धीरे कम करता है।
क्या आत्मज्ञान और ध्यान भी कर्मों के दोषों को मिटाने में मदद करते हैं?
बिल्कुल। आत्मज्ञान (स्वयं को जानना) और ध्यान (मेडीटेशन) वैदिक परंपरा के अभिन्न अंग हैं जो कर्मों के दोषों को मिटाने में अत्यधिक प्रभावी हैं। आत्मज्ञान हमें अपने वास्तविक स्वरूप और कर्मों के क्षणभंगुर स्वभाव को समझने में मदद करता है, जिससे हम आसक्ति और अहंकार से मुक्त होते हैं। ध्यान मन को शांत करता है, जागरूकता बढ़ाता है, और नकारात्मक विचारों व भावनाओं को शुद्ध करता है, जो अंततः कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है।
क्या पूर्व जन्म के कर्मों के दोषों को भी वैदिक उपायों से दूर किया जा सकता है?
वैदिक परंपरा के अनुसार, पूर्व जन्म के संचित कर्मों के फल हमें वर्तमान जीवन में मिलते हैं। हालांकि, वर्तमान में किए गए सत्कर्म (अच्छे कर्म), तपस्या, दान, भक्ति, और ज्ञान की प्राप्ति से इन संचित कर्मों के प्रभावों को कम किया जा सकता है और उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। यह पूर्णतः मिटाना नहीं, बल्कि उनके प्रभाव को क्षीण करना और भविष्य में नए नकारात्मक कर्मों के संचय को रोकना है।









